रस के अवयव
रस के अवयव :-
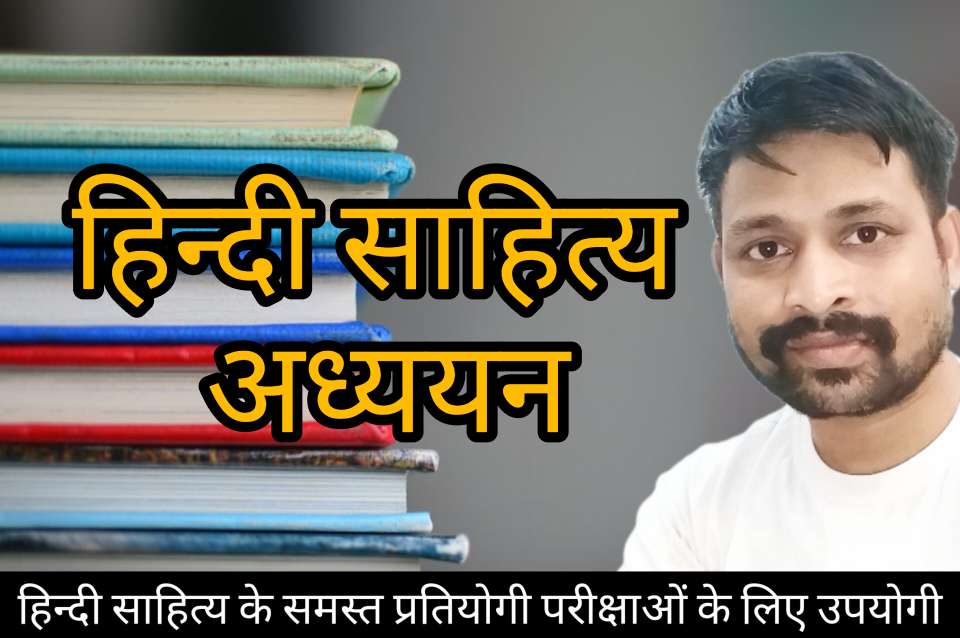
Table of Contents
रस के चार अवयव है-
(1)स्थायी भाव :-
प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कुछ न कुछ भाव अवश्य रहते है तथा वे कारण पाकर जागृत होते है ।उदाहरण -प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुःख, घृणा, शोक, करुणा आदि भाव रहते है।ये एसे भाव है जो संस्कार के रूप मे जन्म लेने के साथ हमारे चित्त मे रहते है।
इसी प्रकार साहित्य में भी इस प्रकार के भाव होते है, इन्हें स्थायी भाव कहते है।उनकी संख्या 9 है-
(1)रति (2)ह्रास (3)शोक (4) क्रोध (5)उत्साह (6)भय (7)विस्मय (8)निर्वेद(वैराग्य या शांति) (9) वात्सल्य (अपने से छोटे के लिये प्रेम)
(2)विभाव :-
रस के कारण को विभाव कहते है।लोक में जो प्रदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उदबोधक है, वे काव्य नाटक आदि में वर्णित होने पर शास्त्रीय शब्दों में विभाव कहलाते है।
यथा- रत्याद्युद् बोधक लोके विभावाः काव्यनाट्ययोः ।
विभाव के दो भेद है –
(1) आलम्बन विभाव –
काव्य-नाटकादि मे वर्णित जिन पात्रो को आलम्बन करके सामाजिक के इत्यादि स्थायी भाव रसरूप में अभिव्यक्त(परिणत) होते है ,उन्हें आलम्बन विभाव कहते है, जैसे – श्रृंगार रस में नायक -नायिका आदि।आलम्बन विभाव के दो भेद है, विषय और आश्रय ।विषय को आलम्बन भी कहते है।जिस पात्र के प्रति किसी के मन मे भाव जागृत होते है वह आश्रय कहलाता है ।उदाहरार्थ – ‘अभिज्ञान सकुन्तलम्’
में दुष्यन्त के मन मे शकुंतला को देखकर भाव-रति भाव -जागृत होता है।शकुंतला को ‘आलम्बन ‘ कहेंगे और दुष्यंत को ‘आश्रय’ ।
(2) उद्दीपन विभाव :-
उद्दीपन विभाव वे कहलाते है जो रस को उद्दीप्त करते है-अर्थात जो रत्यादी स्थायी भावो को उद्दीप्त करके उनकी आस्वादन-योग्यता बढ़ाते है और इस प्रकार उन्हें रसावस्था तक पहुचाने में सहायक होते है।
उद्दीपन विभाव दो प्रकार के माने गए है- (1)आलम्बनगत चेस्टाए (2) वाह्य वातावरण
उदाहरण – श्रृंगार रस में दुष्यन्त(आश्रय) के रतिभाव को अधिक तीब्र करने वाली शकुन्तला (आलम्बन)की कटाक्ष, भुजा-विक्षेप आदि चेस्टाये उद्दीपन विभाव कहलाती है इसी प्रकार श्रृंगार रस में नदी तट, पुष्पवाटिका ,चाँदनी रात इत्यादि वाह्य वातावरण, जोकि आश्रय के स्थायी भावो को उद्दीपन करता है, ‘उद्दीपन विभाव’ कहलाता है।
(3)अनुभाव:-
रत्यादी स्थायी भावो को प्रकाशित करने वाली आश्रय की वाह्य चेस्टाए जो लोक में कार्य कही जाती है, काव्य नाटक में वर्णित अथवा दर्शित होने पर अनुभाव कहलाती है।
यथा –
उद् बुध्दे कारणेः स्वेः स्वैर्बहिर्भावं प्रकाशयन्।
लोके य कार्यरूपः सोअ्नभावः काव्यनाट्ययोः ।।
उदाहरण – विप्रलम्भ श्रृंगार में विरह-व्याकुल नायक द्वारा सिसकिया भरना ,अपने बाल नोचना ,आदि वाह्य चेस्टाए अनुभाव कहलाती है।
अनुभाव के उक्त चार रूपो में से प्रथम तीन अनुभाव ‘यत्नज’ कहलाते है, क्योंकि नाटक में तो इनके निर्वहण में आश्रय को चेस्टा करनी पडती है उदाहरण -क्रुद्ध परशुराम द्वारा कुल्हाड़ी उठाना आदि वाह्य चेस्टाएँँ आंगिक अनुभाव है, आँखे लाल हो जाना आदि सात्विक अनुभाव।
- “”बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौंह करे, भौंहनि हंसे, दैन कहै नटि जाय”” में अनुभाव है?
- – गोपियों की चेष्टाएं, सौंह करे, भौंहनि हंसे आदि अनुभाव है।
- अनुभाव के प्रकार है – 1 कायिक (शारीरिक), 2 मानसिक, 3 आहार्य (बनावटी), 4 वाचिक (वाणी), 5 सात्विक (शरीर के अंग विकार)
- सात्विक अनुभाव की संख्या है – आठ। स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वेपथु, वैवण्य, अश्रु, प्रलय
- नायिका के अनुभाव माने गए है – 28 प्रकार के।
(4)संचारी भाव (व्याभिचारिणी भाव) –
अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तिया ‘संचार भाव’ कहलाती है, ये विकार आश्रय और आलम्बन के मन मे उनमग्न और निर्मग्नहोते रहते है। संचारि शब्द का अर्थ है साथ- साथ चलना तथा संचरणील होना। ये स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले भाव होते है।
संचारी भाव के भेद है – भरत मुनि ने 33 संचारी भाव माने है (निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, देन्य, चिंता, मोह, स्मृति, घृति, ब्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अमर्ष, अविहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, वितर्क) महाकवि देव ने 34 वां संचारी भाव छल माना लेकिन वह विद्वानों को मान्य नहीं हुआ। महाराज जसवंत सिंह ने भारतभूषण में 33 संचारी भावों को गीतात्मक रूप में लिखा है।