परिवर्तन सुमित्रानंदन पन्त सम्पूर्ण कविता व्याख्या
‘परिवर्तन’ यह कविता 1924 में लिखी गई थी। कविता रोला छंद में रचित है। यह एक लम्बी कविता है। यह कविता ‘पल्लव’ नामक काव्य संग्रह में संकलित है। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने एक ‘ग्रैंड महाकाव्य’ कहा है। स्वयं पंत जी ने इसे पल्लव काल की प्रतिनिधि रचना मानते हैं।
परिवर्तन को कवि ने जीवन का शाश्वत सत्य माना है। यहाँ सबकुछ परिवर्तनशील है। इसमें परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण है। परिवर्तन को रोकने की क्षमता किसी में भी नहीं है।
परिवर्तन सुमित्रानंदन पन्त सम्पूर्ण कविता व्याख्या
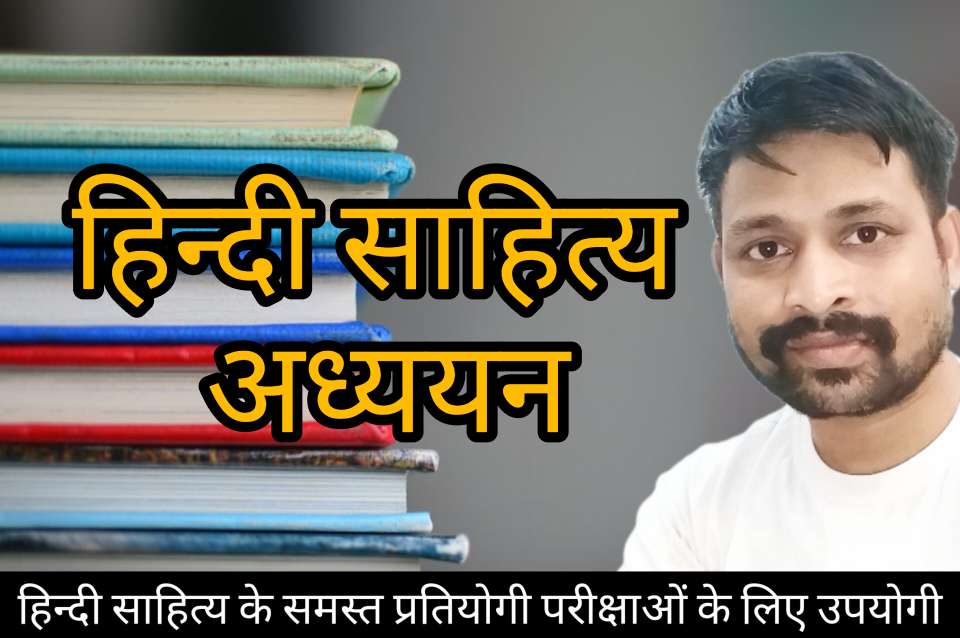
कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन,
वह सुवर्ण का काल ?
भूतियों का दिगन्त छविजाल,
ज्योति चुंबित जगती का भाल ?
राशि- राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार
स्वर्ग की सुषमा जब साभार
धरा पर करती थी अभिसार !
प्रसूनों के शाश्वत शृंगार,
स्वर्ण मृगों के गंध विहार गूँज उठते थे बारम्बार,
सृष्टि के प्रथमोद्गार नग्न सुन्दरता थी सुकुमार,
ऋद्धि औ’ सिद्धि अपार ।
अये, विश्व का स्वर्ण स्वप्न, संसृति का प्रथम प्रभात,
कहाँ वह सत्य, वेद विख्यात ?
दुरित, दुख दैन्य न थे जब ज्ञात,
अपरिचित जरा मरण भ्रूपात !
शब्दार्थ- भूतियों- ऐश्वर्यों का समूह, सुषमा- सौन्दर्य , अभिसार करना – विहार करना, शाश्वत- कभी न अन्त होने वाला, नग्न सुन्दरता-प्राकृतिक सौन्दर्य .
प्रसंग- पंतजी ‘परिवर्तन’ शीर्षक कविता में उस पुरातन वैभव का स्मरण कर रहे हैं, जिसमें नग्न सौन्दर्य विद्यमान था।
केन्द्रीय भाव – विश्व में जब सम्पदा का विकास प्रारम्भ हुआ था, उस समय चारों ओर स्वर्गीय प्राकृतिक सौन्दर्य छाया हुआ था। दिगन्त में भूतियाँ बिखरी हुई थीं। राशि-राशि सद्यता से वसुधा का शृंगार हो रहा था। चारों ओर नग्न सुकुमारता फैली हुई थी। प्रस्तुत प्रसंग में कवि इसी तथ्य का पल्लवन कर रहा है।
व्याख्या – सरल और सौम्य प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण काल अब नहीं है, वह हमारा स्वर्ण युग था। उस समय सारी विभूतियाँ दिशाओं के छोरों तक फैली हुई थीं। संसार में चारों ओर ज्ञान और तेज का प्रकाश था। पृथ्वी के ऊपर प्रत्येक क्षेत्र में विकास था। वसुधा सद्य:यौवन से परिपूर्ण थी। उस समय स्वर्ग का समस्त सौन्दर्य पृथ्वी पर विहार करता था।
प्रसूनों द्वारा धरा का अमर शृंगार होता था। मानव स्वर्ण मृग बने हुए विहार करते थे। सृष्टि के प्रणय से युक्त प्रथम उद्गार वायुमंडल में गूँजा करते थे। सृष्टि के चारों ओर सुकुमार नग्न सौन्दर्य का प्रसार था। उसमें किसी प्रकार की सजावट नहीं आई थी।
उस समय सृष्टि के प्रथम प्रभात में चारों ओर स्वर्णिम स्वप्न व्यापा हुआ था। मानव वेद-विख्यात सत्य की खोज में संलग्न थे। उस समय मानव दुःख, पाप और दीनता की भावना से परिचित भी नहीं था। वृद्धावस्था और मरण का दुख भी मनुष्य को ज्ञात नहीं था। वे कर्त्तव्य का सामना करते हुए शत शरद् देखने की आकांक्षा रखते थे। मृत्यु तो उनके लिए नवीन जीवन में प्रवेश का द्वार मात्र था।
विशेष- (1) कवि वैदिककालीन आदर्श जीवन और वैभव से प्रभावित है। वर्तमान की स्थिति सर्वथा अपने प्रतिकूल देखकर वह आश्चर्यचकित होकर प्रश्न कर उठता है कि
“कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन ?”
(2) अलंकार-‘स्वर्ण की सुषमा’ और ‘सुवर्ण का काल’ में विशेषण विपर्यय ‘राशि-राशि’ में पुनरुक्ति प्रकाश, ‘दुरित’—–दैत्य’ में वृत्यनुप्रास
हाय! सब मिथ्या बात !
आज तो सौरभ का मधुमास
शिशिर में भरता सूनी साँस !
वही मधुऋतु की गुंजित डाल
झुकी थी जो यौवन के भार,
• अकिंचनता में निज तत्काल,
सिहर उठती जीवन है भार!
आज पावस नद के उद्गार
काल के बनते चिह्न कराल ;
प्रातः का सोने का संसार
जला देगी संध्या की ज्वाल,
अखिल यौवन के रंग उभार
हड्डियों के हिलते कंकाल ;
कचों के चिकने, काले व्याल
केंचुली, काँस, सिवार,
गूंजते हैं सबके दिन चार,
सभी फिर हाहाकार !
शब्दार्थ- सौरभ का मधुमास- सुगन्धि का बसन्त, प्राचीन वैभव और सरल सौन्दर्य , सुनी साँस भरना= व्यतीत हो जाना। अकिंचनता – तुच्छता। भार- बोझ , कचों – केशों
प्रसंग-कवि ‘परिवर्तन’ कविता में प्राचीन वैभव और सद्यः सौन्दर्य प्रभात देखकर व्यथित हो रहा है।
केन्द्रीय भाव-संसार मिथ्या है। इसमें परिवर्तन नित्य और शाश्वत है। मधुमास के बाद यहाँ शिशिर आता है। प्रातः का स्वर्णिम संसार संध्या की लालिमा में डूब जाता है तथा यौवन प्रदीप्त शरीर हड्रियों का ढाँचा मात्र रह जाता है। पश्चात् दुःख का पुनः आगमन होता है।
व्याख्या- यह संसार नश्वर है। यह परिवर्तन का चक्र सदैव चलता रहता है। यहाँ सुख के हाहाकार उपस्थित हो जाता है। इस सृष्टि में सभी कुछ मिथ्या है। आज यदि सौरभ से परिपूर्ण वसन्त है तो कल ही शिशिर आकर अपना अधिकार जमा लेता है। बसन्त ऋतु में वृक्ष की डाल पुष्प-राशि से युक्त होकर सौन्दर्य और यौवन के भार से झुकती थी, उस पर पक्षी कलरव करते थे। किन्तु शिशिर में वह पुष्प और पल्लवों से रहित होकर शून्य हो रही है। वह अपनी अकिंचनता पर सिहर उठती है। उसे अपना जीवन भार-सा लगने लगता है।
जहाँ वर्षा के बादल उमड़ते थे, वहाँ जल का प्रभात हो जाता है और काल उस नदी के चिह्न मात्र छोड़ देता है। प्रातः के समय चारों ओर स्वर्णिम आभा छा जाती है, किन्तु संध्या अपनी ज्वाला में उनको जला डालती है।
जो मानव शरीर यौवन से पूर्ण होकर सौन्दर्य की प्रतिमा बन जाता है, वृद्धावस्था आकर उसी शरीर को हड्डियों का ढांचा बना देती है।
जो केश काले नाग की तरह चिकने और सुन्दर होते हैं, वही केंचुली, कांस और सेवार की तरह सौन्दर्यहीन हो जाते हैं। महाकाल सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में परिवर्तन उपस्थित कर देता है।
विशेष-(1) छायावादी प्रतीक शैली है। (2) अलंकार – मानवीकरण, विशेषण विपर्यय तथा उपमा
आज बचपन का कोमल गीत।
जरा का पीला पात!
चार दिन सुखद चाँदनी रात,
और फिर अंधकार, अज्ञात !
शिशिर-सा झर नयनों का नीर
झुलस देता गालों का फूल,
प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर
अधर जाते अधरों को भूल !
मृदुल होठों का हिमजल ह्रास
उड़ा जाता निःश्वास समीर,
सरल भौंहों का शरदाकाश
घेर लेता, घन, घिर गम्भीर !
शून्य साँसों का विधुर वियोग
छुड़ाता अधर मधुर संयोग;
मिलन के पल केवल दो, चार,
विरह के कल्प अपार !
अरे, वे अपलक चार नयन
आठ आँसू रोते निरुपाय;
उठे रोओं के आलिंगन
कसक उठते काँटों से हाय !
शब्दार्थ- निरुपाय = उपायरहित ।
प्रसंग – प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी सृष्टि के असीम विरह की झाँकी दिखा रहे हैं।
केन्द्रीय भाव- सृष्टि में परिवर्तन शाश्वत है। परिवर्तन के चक्र से जड़-चेतन कोई भी नहीं बचता। यहाँ क्षणिक मिलन के उपरान्त चिर वियोग हो जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि इसी तथ्य का पल्लवन कर रहा है।
व्याख्या- सृष्टि में पल-पल में परिवर्तन हो रहा है। बालक का सुकुमार कोमल शरीर वृद्धावस्था में पीले पत्ते की तरह हो जाता है। चाँदनी रात चार दिन को ही रहती है और उसके पश्चात् अज्ञात अँधेरा ही अँधेरा छा जाता। है। मनुष्य की जीवन-सन्ध्या में शिशिर में पाला या ओस के समान अश्रु प्रवाहित होकर गालों के फूलों को मुरझा देते हैं। जिस प्रकार शरद् ऋतु में फूल मुरझा जाते हैं, उसी प्रकार से बुढ़ापा आते ही गालों में झुर्रियाँ पड़ जाती है। जिन गालों की उपमा गुलाब से दी जाती है, वे मुरझा जाते हैं। जवानी में जो अधर प्रणयी का चुम्बन लेने के लिए रहते थे, वे अपनी दशा भूल जाते हैं अर्थात् या तो वे सूख जाते हैं या विकृत होकर लटक पड़ते हैं।
जिन कोमल होठों से हिमजल-सा मधुर हास प्राय: बिखरता था, उन्हीं से अब ठण्डी आहे निकल रही हैं। जो भौहें सुन्दर शरदाकाश की तरह थीं उनको बुढ़ापे में चिन्ता के बादल घेर लेते हैं। मनुष्य की चैतन्यता शून्य-सी हो जाती है, अब वह अधरामृत पान की भी आकांक्षा नहीं करता।
इसीलिए यह सत्य है कि इस संतृप्ति में मिलन के तो दो-चार पल ही आते हैं, किन्तु यहाँ विरह अपार कल्पों के समान है। जो नेत्र प्रिया के नेत्रों से मिलकर अपलक होकर सौन्दर्य का पान करते थे और कभी भी थकते नहीं थे, आज वे निरुपाय होकर आँसू बहा रहे हैं। प्रिया से आलिंगन करते समय रोमांच होने से जो रोयें खड़े होकर आनन्द को प्रकट करते थे, वे अब कंटक के समान पीड़ा देते हैं
“मिलन के पल केवल दो चार,
विरह के कल्प अपार ।”
विशेष- (1) मुहावरों का सफल काव्यात्मक प्रयोग तथा छायावादी प्रतीक शैली है। (2) अलंकार तथा उपमा अलंकार है।
किसी को सोने के सुख साज
मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज;
चुका लेता दुख कम ही ब्याज
काल को नहीं किसी की लाज !
विपुल मणि रत्नों का छवि जाल,
इन्द्रधनु की-सी छटा विशाल
विभव की विद्युत ज्वाल चमक,
छिप जाती है तत्काल ;
मोतियों जड़ी ओस की डार
हिला जाता चुपचाप बयार !
शब्दार्थ- बयार हवा ।
प्रसंग-प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी परिवर्तन को महान् शक्ति के रूप में देख रहे हैं।
केन्द्रीय भाव-कवि स्पष्ट करना चाहता है कि संसार का सुख क्षणिक है, किन्तु दुःख चिर और व्यापक है।
व्याख्या- संसार में किसी को भी स्थायी सुख नहीं मिलता। यदि आज किसी को क्षणिक सुख मिल भी जाता है तो वह इस प्रकार होता है, जैसे कि उधार लिया हुआ धन हो। जिस प्रकार उधार देने वाला महाजन ऋणियों से ब्याज सहित धन वसूल कर लेता है, उसी तरह से कालरूपी परिवर्तन क्षणिक दिए हुए सुख के बदले में अपार दुःख देता है। संसार में वैभव और चमक-दमक की चपला क्षणमात्र में छिप जाती है। तरह-तरह के अनेकों रत्न माणिक्य’ और सौन्दर्य इन्द्रधनुष की तरह दिखाई देकर क्षण मात्र में छिप जाते हैं।
जिस प्रकार ओस भरी डाल को हवा का झोंका हिलाकर शून्य कर देता है, उसी प्रकार से परिवर्तन का एक झौंका मानव के समस्त वैभव को समेटकर ले जाता है।
विशेष- अलंकार- उपमा और दृष्टान्त ।
खोता, इधर जन्म लोचन
मूंदती उधर मृत्यु क्षण-क्षण,
अभी उत्सव औ’ हास हुलास
अभी अवसाद अश्रु, उच्छ्वास।
अचिरता देख जगत् की आप
शून्य भरता समीर निःश्वास
डालता पातों पर चुपचाप
ओस के आँसू नीलाकाश;
सिसक उठता समुद्र का मन,
सिहर उठते उडगन ।
शब्दार्थ- अवसाद दुःख अचिरता नश्वरता।
प्रसंग- प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार की नश्वरता को देखकर प्रकृति भी आँसू गिराती है।
व्याख्या- संसार में एक ओर दुःख है तो दूसरी ओर सुख है। एक ओर जन्म होता है तो दूसरी ओर मृत्यु का तांडव नृत्य होता है। अभी जहाँ पर प्रसन्नता और हास-विलास होता है, वहाँ पर तत्काल ही अवसाद और अश्रु का वातावरण छा जाता है। संसार की इस नश्वरता को देखकर पवन भी शून्य में ठण्डी साँसें भरता है। पत्तों के ऊपर ओस के रूप में चुपचाप अपने आँसू गिराता है तथा समुद्र का मन भी सिसकियाँ भरने लगता है। और तारागण सिहर उठते हैं।
अहे दुर्जेय विश्वजित् !
नवाते शत सुरवर, नरनाथ
तुम्हारे इंद्रासन तल माथ;
घूमते शत-शत भाग्य अनाथ,
सतत रथ के चक्रों के साथ।
तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित;
करते हो संसृति को उत्पीड़ित, पद मर्दित,
नग्न नगर कर, भग्न भवन, प्रतिमायें खंडित,
हर लेते हो विभव, कला, कौशल, चिर संचित !
आधि, व्याधि, बहुवृष्टि, वाता, उत्पात, अमंगल
वह्नि, बाढ़, भूकम्प – तुम्हारे विपुल सैन्य दल,
अहं निरंकुश ! पदाघात से जिनके विह्वल
हिल हिल उठता है टल-मल
पददलित धरातल ।
प्रसंग – प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी परिवर्तन का वर्णन दुर्जेय शक्ति के रूप में कर रहे हैं।
केन्द्रीय भाव- परिवर्तन के समक्ष संसार की महान् से महान् शक्ति विनत हो जाती है। परिवर्तन कभी निरंकुश नृपति की तरह अत्याचार करता है और कभी सृष्टि का विनाश करते हुए मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं को जन्म देता है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि इसी तथ्य को पल्लवित कर रहा है।
व्याख्या- हे परिवर्तन ! तुम विश्वविजयी हो। तुमको संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे इन्द्रासन के नीचे आकर सैकड़ों देवता और नृपति शीश झुकाते हैं। तुम्हारे कठोर चक्र में फँसकर सैकड़ों भाग्यशाली अनाथ होकर भटकते फिरते हैं।
तुम क्रूर और अत्याचारी राजा की तरह अनियन्त्रित रूप से संसार को कुचलने लगते हो। तुम्हारे आक्रमण से नगर के नगर उजड़ जाते हैं, महल खण्डहर हो जाते हैं और संस्कृति के प्रतीक • कला-कौशल आदि जो चिरकाल से संचित थे, वे सभी नष्ट हो जाते हैं।
हे परिवर्तन ! तुम्हारा सैन्य दल भी तुम्हारी तरह क्रूर और अत्याचारी है। मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बहु-वृष्टि, झंझावात, उपद्रव, अमंगल, अग्नि, बाढ़, भूकम्प आदि तुम्हारी सेना के क्रूर सैनिक है, जिनके पैरों के आघात से ही धरातल पद-दलित बना हुआ टलमल-टलमल करते हुए हिलने लगता है।
विशेष- (1) रस-यहाँ परिवर्तन का वर्णन स्थायी भाव ‘भय’ को उद्दीप्त कर रहा है, इसलिए भयानक रस है।
(2) अलंकार – परिवर्तन की समानता नृशंस नृपति से होने के कारण उपमा, ‘ आधि, व्याधि दल’ में सैन्य दल का आरोप होने से रूपक तथा ‘ हिल-मिल’ में पुनरुक्तिप्रकाश
अहे निष्ठुर परिवर्तन !
तुम्हारा ही तांडव नर्तन
विश्व का करुण विवर्तन !
तुम्हारा ही नयनोन्मीलन,
निखिल उत्थान पतन !
लक्ष अलक्षित चरण तुम्हारे चिह्न निरन्तर
छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्षः स्थल पर !
शत-शत फेनोच्छ्वसित, स्फीत फूत्कार भयंकर
घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर ।
मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक, कल्पांतर,
अखिल विश्व ही विवर,
वक्र-कुंडल दिङ्मंडल।
शब्दार्थ- विवर्तन – विश्व का विभिन्न स्थितियों को पार कना। नयनोन्मीलन- नेत्रों का खुलना। निखिल- सम्पूर्ण , विक्षत- घायल, बुरी तरह कटा-पिटा, फेनोच्छ्वसित- फेनयुक्त, उच्छ्वास . स्फीत = प्रसार, घना, मोटा, भयंकर अत्यधिक . गरल दन्त – विष का दाँत , कंचुक -बदलना। कल्पान्तर – एक कल्प व्यतीत होकर दूसरा आना।
प्रसंग – प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी परिवर्तन का वर्णन विश्व की महाशक्ति के रूप में कर रहे हैं।
केन्द्रीय भाव- परिवर्तन समस्त सृष्टि को नियन्त्रित किए हुए है। यही विश्व के उत्थान-पतन का कारण है। परिवर्तन ही सहस्र फन वाले वासुकि की तरह दिङ्मण्डल में मारे बैठा हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग में कवि इसी भाव को पल्लवित कर रहा है।
व्याख्या- हे परिवर्तन ! तुम सृष्टि की निष्ठुर महाशक्ति हो। विश्व में जितनी स्थितियाँ आती हैं, वे तुम्हारे तांडव नृत्य के कारण ही आती है तुम्हारे ही नेत्रों को खोलने विश्व का उत्थान और पतन होता है।
हे परिवर्तन ! तुम सहस्र फन वाले वासुकि नाग हो। जिस प्रकार सर्प अपने अल चरण-चिह्न छोड़ता चलता है, उसी प्रकार से संसार के बुरी तरह से घायल हृदय पर तुम भी अपना प्रभाव छोड़ देते हो। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है, वह होता रहता है; किन्तु दिखाई नहीं। पड़ता। तुम्हारे फेन से युक्त उच्छ्वास अत्यन्त विनाशकारी है। तुम्हारी घनी फूत्कारअन भयंकर हैं। तुम अपनी किंचितमात्र उच्छ्वास से ही संसार में विनाशकारी दृश्य उपस्थित कर देते हो। तुम्हारे ही संकेत से यह आकाश घनाकार होकर घूम रहा है।
हे वासुकि रूप परिवर्तन) तुम्हारे गरल-दन्त मृत्यु है। जिस प्रकार वासुकि का काटा हुआ नहीं बचता, उसी प्रकार से मृत्यु से संसार की रक्षा नहीं होती। जिस प्रकार सर्प अपनी पुरानी कॅचुली उतारकर नई धारण करता है .उसी प्रकार से तुम युग परिवर्तन करते रहते हो। सम्पूर्ण विश्व ही तुम्हारे रहने के लिए विका (बिल) है और दिङ्मंडल ही वक्र कुण्डली है।
जगत् का अविरत हृत्कम्पन
तुम्हारा ही भयसूचन;
निखिल पलकों का मौन पतन
तुम्हारा ही आमंत्रण !
विपुल वासना विकच विश्व का मानस शतदल
छान रहे तुम, कुटित काल कृमि से घस पल-पल;
तुम्हीं स्वेद सिंचित संसृति के स्वर्ण शस्य दल
दलमल देते, वर्षोपल बना, वांछित कृषिफल !
अये, सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिङ्मंडल
नैश गगन-सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल!
शब्दार्थ- अविरल – लगातार. हृत्कम्पन – हृदय की धड़कन । विकच = विकसित। कृमि – कीड़ा। वर्षोपल- वर्षा के साथ गिरने वाले भीषण ओले।
प्रसंग -प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी परिवर्तन का भीषण विनाशक शक्ति के रूप में वर्णन कर रहे हैं।
व्याख्या—हे परिवर्तन ! तुम्हारे ही भय से संसार का हृदय निरन्तर धड़का करता है। तुम्हारे ही आमन्त्रण पर भय के कारण समस्त सृष्टि के पलक नीरवता से घिर जाते हैं। विश्व के मनुष्यों का हृदय-कमल, जो नाना प्रकार की इच्छाओं से युक्त है, उसे तुम जटिल-कालरूपी कोट बनकर पल मात्र में काट देते हो।
मनुष्य अपने पसीने से सींचकर हरी-भरी खेती तैयार करते हैं, किन्तु तुम उस खेती को ओलों की वर्षा करके नष्ट कर देते हो। तुम्हारी भाग्यपूर्ण ध्वनि से संसार की समस्त दिशा शब्दायमान हो रही हैं। यह अन्धकारमय समस्त आकाश तुम्हारा ही समाधि-स्थल है।
2) अलंकार- उल्लेख, रूपक, उपमा, वृत्यनुप्रास तथा छेकानुप्रास
काल का अकरुण भृकुटि विलास
तुम्हारा ही परिहास,
विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास !
तुम्हारा ही इतिहास !
एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयकर
समर छेड़ देता निसर्ग संसृति में निर्भर!
भूमि चूम जाते अभ्रध्वज सौध, शृंगवर,
नष्ट-भ्रष्ट साम्राज्य – मूर्ति के मेघाडम्बर!
अये, एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकम्पन,
गिर- गिर पड़ते भीत पक्षि पोतों से उड्डुगन !
आलोड़ित अंबुधि फेनोन्नत कर शत-शत फन,
मुग्ध भुजंगम-सा, इंगित पर करता नर्तन ।
दिक् पिंजर में बद्ध, गजाधिप-सा वनितानन !
वाताहत हो गगन
आर्त करता गुरु गर्जन।
शब्दार्थ- अकरुण -क्रूर और कठोर, परिहास – हँसी. निसर्ग- प्रकृति, अभ्रध्वज – बादल ही जिनकी ध्वजायें हैं। पोतों -बच्चों। आलोड़ित -मथा हुआ-सा | विनतानन = मुख नीचा किए हुए।
प्रसंग – प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी परिवर्तन के प्रलयंकारी रूप का वर्णन कर रहे हैं।
केन्द्रीय भाव- परिवर्तन का एक कुटिल-कटाक्ष ही संसार में प्रलय प्रारम्भ कर देता है। इसी तथ्य को कवि प्रस्तुत प्रसंग में पल्लवित कर रहा है। ?
व्याख्या – हे परिवर्तन ! काल जो अपनी क्रूर भुकुटी तानता है, उसमें तुम्हारा ही परिहास है। तुम्हारे द्वारा ही विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास लिखा जाता है। तुम्हारा एक कठोर कटाक्ष ही महान् प्रलयंकारी है। वह प्रकृति और सृष्टि में विनाश का तांडव-नृत्य प्रारम्भ कर देता है। जो भवन आसमान तक ऊँचे हैं, तुम्हारे एक संकेत से पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पर्वत की चोटियाँ टूट-टूटकर गिरने लगती हैं। जिस प्रकार हवा से बादलों के झुण्ड बिखर जाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे कठोर कटाक्ष से साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं।
हे परिवर्तन! तुम्हारा एक रोमांच ही दिशाओं को कँपा देता है। तारे टूट-टूटकर आकाश से इस प्रकार गिरने लगते हैं, जिस प्रकार से वृक्ष के कोटर से पक्षियों के बच्चे भयभीत होकर गिर पड़ते हैं। तुम्हारे किंचित रोमांच से ही समुद्र मथ जाता है और वह फेनोच्छ्वास के रूप में शत-शत फन उठा देता है एवं भूजंग के समान मुग्ध बना हुआ तुम्हारे सकेत पर नृत्य करता है। तुम्हारे कठोर कटाक्ष से आकाश भी काँप उठता है। वह दिशाओं के पिंजरे में बन्द होकर गजराज के समान मुँह नीचा किय हुए पवन से आहत होकर आर्त स्वर में गुरु-गर्जना करने लगता है।
विशेष-
(1) रस- परिवर्तन के प्रलयकारी रूप में उपस्थित होने के कारण भय स्थायीभाव उद्दीप्त होता है, अतः भयानक रस है।
(2) अलंकार परिवर्तन का अनेक प्रकार से वर्णन होने के कारण उल्ले ‘कठोर-कटाक्ष’ में ‘क’ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने छेकानुप्रास ‘गिरि-गिरि पुनरुक्तिप्रकाश, ‘आलोड़ित अम्बुधि’ की ‘मुग्ध भुजंगम’ से समता तथा ‘आकाश’ की समत ‘गजाधिप’ से होने के कारण उपमा तथा ‘शत-शत’ में पुररुक्तिप्रकाश।
जगत की शत कातर चीत्कार
बेघतीं बधिर! तुम्हारे कान!
अश्रु स्त्रोतों की अगणित धार!
सींचतीं उर पाषाण!
अरे क्षण सौ-सौ निःश्वास
छा रहे जगती का आकाश!
चतुर्दिक पहर घहर आक्रांति
ग्रस्त करती सुख शांति ।
शब्दार्थ- बधिर – बहरे, आक्रांति- चारों और से होने वाला विप्लव ।
प्रसंग –प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी स्पष्ट कर रहे हैं कि परिवर्तन की विनाश-लीला सम प्रकृति और सृष्टि को आक्रान्त कर रही है।
व्याख्या – हे परिवर्तन ! तुम्हारे क्रूर अत्याचारों और विनाश के तांडव नृत्य से संसर करुणा से भरी चीत्कार कर रहा है; किन्तु वह तुम्हारे मूक कानों को बेधने में समर्थ नहीं है। आज संसार के मनुष्यों के नेत्रों से अश्रु की धारायें प्रवाहित हो रही हैं; किन्तु उससे भी सिंचकर तुम्हारा पाषाण हृदय कोमल नहीं होता।
क्षण मात्र में तुम्हारे शत-शत प्रलयकारी निश्वास निकलकर संसार के आकाश में छा रहे है। तुम्हारे क्रूर तांडव नृत्य के कारण चारों ओर से होने वाला विप्लव सुख-शांति को ग्रस का समाप्त कर रहा है।
विशेष- अलंकार उल्लेख ।
हाय री दुर्बल भ्रांति !
कहाँ नश्वर जगती में शांति !
सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति !
जगत अविरत जीवन संग्राम,
स्वप्न है यहाँ विराम
एक सौ वर्ष, जगर उपवन,
एक सौ वर्ष, विजन वन!
यही तो है असार संसार,
सृजन सिंचन पालन संहार !
आज गर्वोन्नत हर्म्य अपार
रत्न दीपावलि, मंत्रोच्चार;
उलूकों के कल भग्न विहार,
झिल्लियों की झनकार !
दिवस निशि का यह विश्व विशाल
मेघ मारुत का माया जाल।
प्रसंग – प्रस्तुत प्रसंग में पन्तजी असार संसार में परिवर्तन की नित्यता का वर्णन कर रहे हैं
केन्द्रीय भाव- यह संसार नश्वर है, मनुष्य को जीवन संग्राम में एक क्षण की भी शान्ति नहीं मिलती। सृष्टि में सदैव ही परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। सुख और दुःख की आँख मिचौनी खेलता हुआ विश्व आगे को बढ़ता रहता है। इसी तथ्य का प्रस्तुत प्रसंग में पल्लवन है।
व्याख्या- इस संसार में सुख और शान्ति की खोज करना भ्रान्तिमात्र है। इस नश्वर विश्व में शान्ति नहीं है। वास्तव में समस्त सृष्टि ही अशान्ति से परिपूर्ण है। यह संसार निरन्तर रूप से चलता हुआ जीवन-संग्राम है। यहाँ पर विराम और विश्राम स्वप्न में भी नहीं मिल सकता।
सृष्टि में सदैव ही परिवर्तन का चक्र चलता रहता है। एक शताब्दी में जहाँ नगर और उपवन होते हैं, दूसरी में वहाँ पर विजनता और खण्डहर हो जाते हैं। इस असार संसार का क्रम भी यही है। एक ओर यहाँ सृजन होता है, तो दूसरी ओर पतन और यहाँ जो जन्म धारण करता है, वह वनाश को भी अवश्य प्राप्त होता है। आज जहाँ पर ऊँचे-ऊँचे महल गर्व से अपना सिर ऊँचा उआए हुए खड़े हैं, जिनमें रात को दीपकों का प्रकाश और मन्त्रोच्चर हो रहा है, कल वहाँ उलूकों का विहार होगा और झींगुर झनकार करते हुए नीरवता को गम्भीरता प्रदान करेंगे।
“यह विशाल विश्व मेघ और मारुत का मायाजाल है। जिस प्रकार से बादल को मारुत उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार से काल इस नश्वर संसार को नष्ट कर देता है।
विशेष-(1) दिवस विशाल- पन्तजी संसार में दुःख और सुख दोनों की स्थिति मानते हैं।
(2) ‘संसार नश्वर है’- इस शाश्वत सत्य को कवि स्पष्ट कर है।
(3) अलंकार – वीप्सा, छेकानुप्रास तथा उल्लेख ।
अरे, देखो इस पार
दिवस की आभा में साकार
दिगम्बर, सहम रहा संसार ?
हाय ! जग के करतार !!
प्रात ही तो कहलाई माता
पयोधर बने उरोज उदार
मधुर उर इच्छा को अज्ञात
प्रथम ही मिला मृदुल आकार;
छिन गया हाय ! गोद का बाल
गड़ी है बिना बाल की नाल !
शब्दार्थ- सहम रहा -भयभीत हो रहा है।उरोज- युवती के कठोर एवं पीन कुच। पयोधर- शिशु के जन्म देने पर युवती माता बनती है उसके उरोजों में दूध आ जाता है और में ‘पय को धारण करने वाले’ होकर ‘पयोधर’ की संज्ञा पाते हैं।
प्रसंग- इस प्रसंग में कवि परिवर्तन का सुखद और क्रूर चित्र प्रस्तुत करता हुआ कह रहा है।
व्याख्या- तनिक उस ओर दृष्टि डालकर देखो, जहाँ कि दिशाओं से आवृत्त होकर भी आकाश शून्य मात्र लगता है और उसकी इस शून्यता से संसार भयभीत हो रहा है। हे जगत् के विधाता ! तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। काल का क्रूर विधान बनाने वाले तुम कितने निर्दयी हो।
जिस युवती ने अभी यौवन की प्रातः वेला में प्रवेश ही किया था और उसके शिशु उत्पन्न हुआ था, जिससे वह माता कहलायी थी। माता बनते ही उसके उरोजों ने पयोधरों का रूप धारण किया था और दूध धारण करने के कारण उनका पयोधर नाम सार्थक हुआ था। जिसके हृदय की मधुर इच्छा ही शिशु के रूप में मूर्तिमती हुई थी, उसके नवजात शिशु को तुमने सदा के लिए छीन लिया। वह बाला अब जड़ से छिन्नलता के समान व्याकुल पड़ी है।
विशेष-(1) यहाँ शिशु के जन्म और मृत्यु का कवि ने करुणापूर्ण काल्पनिक वर्णन किया है।
(2) अलंकार – ‘हाय जग के करतार’ और ‘छिन गया हाय, गोद का लाल’ में गम्भीर करुणा की अनुभूति वीप्सा अलंकार में व्यक्त हुई है।
अभी तो मुकुट बँधा था माथ,
हुए कल ही हल्दी के हाथ;
खुले भी न थे लाज के बोल,
खिले भी न थे चुम्बनशून्य कपोल ;
बना सिंदूर अंगार;
हाय ! रुक गया यहीं संसार
वातहत लतिका वह सुकुमार
पड़ी है छिन्नाधार !
शब्दार्थ- हल्दी के हाथ – विवाह होना। वात-हत हवा से गिराई हुई। छिन्नाधार =जिसका आधार नष्ट हो गया हो।
प्रसंग – इस प्रसंग में क्रूर परिवर्तन के चक्र में सद्यःविधवा युवती की करुण दशा का चित्र कवि प्रस्तुत कर रहा है।
व्याख्या- उस नवयुवती का अभी कल ही विवाह हुआ था। अभी कल ही वर ने माथे पर मुकुट बाँधकर उससे विवाह किया था और उसके हल्दी से हाथ पीले हुए थे। अभी लज्जा त्यागकर वह पति से दो बातें भी नहीं कर पाई थी, अभी पति के चुम्बनों से उसके कपोल भी शून्य ही थे। वह नव परिणीता विधवा हो गई। पति की मृत्यु हो जाने से उसका सारा सुख-स्वप्न समाप्त है।
हे निष्ठुर विधाता ! उसकी कितनी दयनीय स्थिति है। उसकी माँग का सिंदूर अब दहकता हुआ अगारा बन गया है। पति की मृत्यु ने उसकी मांग का सिंदूर धो दिया है। अब उसकी दशा उस आश्रयहीन लता के समान है, जो तेज आँधी के कारण वृक्ष के नष्ट हो जाने पर गिर पड़ती है और उसका कोई सहारा नहीं रहता।
विशेष-
(1) यहाँ रसात्मक अनुभूति का बिम्ब उपस्थित हो गया है।
(2) मुहावरों के काव्यात्मक प्रयोग के कारण लाक्षणिकता है।
(3) अलंकार-‘हाय’ में ‘वीप्सा’ तथा ‘विधवा’ में ‘वात-हत लतिका’ का आरोप होने से रूपक।
काँपता उधर दैन्य निरुपाय,
रज्जु-सा, छिद्रों का कृशकाय !
न उर में गृह का तनिक दुलार,
उदर ही में दानों का भार !
भूँकता सिड़ी शिशिर का श्वान
चीरता हरे ! अचीर शरीर
न अधरों में स्वर, तन में प्राण,
न नयनों ही में नीर !
शब्दार्थ- निरुपाय = असहाय, रज्जु -रस्सी , कृशकाय = दुर्बल शरीर, दुलार प्यार, अचीर -नग्न, वस्त्र से रहित। नीर-जल
प्रसंग – इस प्रसंग में कवि मानवता का करुण यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर रहा है।
व्याख्या – इस संसार में एक ओर मानवता कराह रही है। ऐसे बहुत से दुःखी जन हैं, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं हैं और जो सर्दी के कारण काँपते रहते हैं तथा शीत के कारण उनका शरीर रस्सी के समान ऐंठा रहता है। उनको भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। वे इतने दुर्बल हो गये हैं कि उनके शरीर में छिद्र से पड़ते जा रहे हैं। वे पेट में दोनों (भोजन) का ही भार ढो रहे हैं। अर्थात् पेट भरने के लिए भोजन तक पाने के लिए वे विवश हैं।
उनके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। उनको सदैव पेट ही की चिन्ता सताती रहती है, उनके वस्त्रहीन नग्न शरीर को देखकर शिशिर ऋतुरूपी श्वान बार-बार भूँककर दाँत गड़ाकर उनके शरीर को चीरने लगता है। उनके अधरों पर न तो कोई स्वर है और न तन में प्राण ही हैं। उनकी आँखों का पानी तक सूख गया है। भाव यह है कि दीनता की अवस्था ने उनको इतना अधिक विवश बना दिया है कि वे कों को सहन करते हुए आँसू तक नहीं बहा सकते।
विशेष-(1) लाक्षणिकता की व्यंजना है। (2) अलंकार-मानवीकरण, ‘रज्जु-सा छिद्रों का कृश गात’ में उपमा, शिशिर में ‘श्वान’ का आरोप होने से रूपक तथा अनुप्रास
सकल रोओं से हाथ पसार
लूटता इधर लोभ गृह द्वार;
उधर वामन डग स्वेच्छाचार;
नापता जगती का विस्तार;
टिड्डियों-सा छा अत्याचार
चाट जाता संसार।
शब्दार्थ- रोओं -शरीर के रोम , वामन डग स्वेच्छाचार – स्वेच्छाचार बावन डग भरता हुआ प्रसार करता जा रहा है।
प्रसंग – इस प्रसंग में कवि विश्व में व्याप्त लोभ, स्वेच्छाचार और अत्याचार के भीषण प्रसार का वर्णन कर रहा है।
व्याख्या- इस विश्व में लोभी शोषक वर्ग है, जिसका रोम-रोम दूसरों का घर द्वार लूटने में संलग्न है। इसकी लूट से मानवता दयनीय स्थिति को प्राप्त होती जा रही है। दूसरी ओर स्वेच्छाचार वामन की तरह डग भरता हुआ विश्व में अपना विस्तार करता जा रहा है। जिस प्रकार टिड़ियों का दल हरी-भरी फसल चाट जाता है, उसी प्रकार अत्याचार विस्तृत होकर संसार को ध्वस्त करता चला जा रहा है।
विशेष-(1) उधर वामन संसार- भगवान् ने बावन (बौना अर्थात् 52 अंगुल के) रूप धारण करके राजा बलि को छला था। उन्होंने राजा बलि से तीन पग पृथ्वी माँगी थी और देने का वचन लेकर नापते समय विराट् रूप धारण करके तीन पगों में तीनों लोकों को नाप लिया था। कवि कहना चाहता है कि आज संसार में बावन डग के समान ही बढ़ता हुआ स्वच्छाचार मानवता को निगले जा रहा है।
(2) ‘रोओं का हाथ पसारना’, ‘लोभ का गृह-द्वार लूटना’, ‘स्वेच्छाचार का डग भरना आदि में मानवीय क्रियाओं का निरूपण किया गया है। अलंकार- ‘विशेष्य’ के स्थान पर ‘विशेषणों’ का कार्य करना वर्णित होने से विशेषण-विपर्यय ‘रोओं’ में ‘हाथ’ का तथा ‘स्वेच्छाचार’ में ‘वामन-डग’ का आरोप होने से रूपक तथा ‘अत्याचार’ की समानता ‘ टिड्डी दल’ से होने में उपमा ।
बजा लोहे के दंत कठोर
नचाती हिंसा जिह्वा लोल ;
भृकुटि के कुंडल वक्र मरोर
फुहुँकता अंध रोष फन खोल !
लालची गीधों से दिन-रात,
नोंचते रोग शोक नित गात,
अस्थिपंजर का दैत्य दुकाल
निगल जाता निज बाल !
शब्दार्थ- लोहे के दन्त -लोहे के अस्त्र-शस्त्र । लोल- चंचल ,वक्र -टेढ़े। फुहुँकता – फुफकारता है। गात -शरीर . दुकाल- बुरा समय
प्रसंग – इस प्रसंग में कवि ने विश्वव्यापी अस्त्रों की संहार लीला और भीषण हिंसा का वर्णन किया है।
व्याख्या – आज भीषण हिंसा अपनी चंचल जिह्वा लपलपाती हुई लोहे के कठोर दाँत बजा रही है। विश्व में हिंसा इतने भीषण स्तर पर व्याप्त हो रही है कि मनुष्य अस्त्र-शस्त्रों से भीषण संहार में लगा हुआ है। अस्त्र-शस्त्र ही लोहे के कठोर दन्त हैं। यह रोषरूपी विपधर सर्प अन्धा होकर फुफकार रहा है। उसकी रोष से भरी हुई भृकुटियाँ ही वक्र कठोर कुण्डल हैं। जिस प्रकार लालची गृद्ध (गोध) प्राणियों के शरीर का माँस नोंच-नोंचकर खाते रहते हैं.
उसी प्रकार यहाँ विविध रोग और शोक नित्य ही दिन-रात लोगों का तन-मन नोंच रहे हैं। अर्थात् विश्व का एक वर्ग मानसिक और शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त है। अस्थि-पिंजररूपी राक्षसी मनुष्यों का विनाश कर देती है। सुधा से ग्रसित मनुष्य अपनी सन्तान का संहार उसी प्रकार कर देते है, जिस प्रकार दैत्य स्वयं अपनी सन्तान को मार डालते हैं।
विशेष- (1) ‘बजा लोहे के दन्त’ में लाक्षणिकता व्यंजित हैं। (2) अलंकार-‘भृकुटि’ में ‘वक्र कुण्डल’ और ‘रोष’ में सर्प’ का आरोप होने से रूपक एवं रोग-शोक’ की समानता गीतों’ से की जाने से उपमा (अमूर्त उपमेय के लिए मूर्त उपमान की योजना है।
बहा नर शोणित मूसलाधार,
रुंड मुंडों की कर बौछार,
प्रलय घन-सा फिर भीमाकार
गरजता है दिगन्त संहार;
छेड़कर शस्त्रों की झनकार
महाभारत गाता संसार ।
कोटि मनुजों के निहित अकाल
नयन मणियों से जटित कराल,
अरे, दिग्गज सिंहासन जाल,
अखिल मृत देशों के कंकाल;
मोतियों के तारक लड़ हार
आँसुओं के शृंगार !
शब्दार्थ- शोणित = रक्त । भीमाकार- बहुत भयावने आकार का।
प्रसंग- इस प्रसंग में कवि विश्व में व्याप्त भीषण रक्तपात और संहार का वर्णन कर रहा है।
व्याख्या – मनुष्य इतना क्रूर, हिंसक और रक्त पिपासु हो गया है कि वह मनुष्य के रक्त की मूसलाधार धारा बाहाने में संलग्न है। उसकी भीषण हिंसा में रुण्ड मुण्डों की बौछार हो रही है। आज समस्त दिशाओं में प्रलय का भीमाकार घन घिरकर गर्जना कर रहा है।
आज हिंसक क्रूर संसार भीषण संहारक अस्त्रों की झंकार करता हुआ महाभारत अर्थात् भीषण मार-काट मचाये हुए है। इस विश्व में विशाल सिंहासन और राज्य असंख्य मृत पुरुषों के कंकालों पर खड़े हुए हैं। रक्तपिपासु मनुष्य ने अपना राज्य बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करके भीषण नरसंहार किया- उनकी नेत्र-मणियों से ही उनके सिंहासन जटित हैं। इस क्रूर और
हिंसक विश्व में मोतियों के तारक खेड़ियों के हार अश्रुओं के शृंगार मात्र हैं।
विशेष-(1) अमूर्त उपमेय के लिए मूर्त उपमान की योजना सम्पूर्ण छन्द में है।
(2) ‘संसार का महाभारत गान’ में लाक्षणिक प्रयोग है।
(3) अलंकार- ‘नयन मणियों’, ‘दिग्गज कंकाल’, ‘संहार’ की समानता ‘प्रलय के घन’ से होने में उपमा, मोतियों…… शृंगार’ में रूपक।
रुधिर के हैं जगती के प्रात,
चितानल के ये सायंकाल;
शून्य निःश्वासों के आकाश,
आँसुओं के ये सिंधु विशाल ।
यहाँ सुख सरसों, शोक सुमेरु,
अरे, जग है जग का कंकाल !!
वृथा रे ये अरण्य चीत्कार,
शांति सुख है उस पार ।
शब्दार्थ- चितानल- चिंता की अग्नि , अरण्य = वन, सुनसान,.चीत्कार- चीख-चीखकर रोना।
प्रसंग – कवि को संसार की भीषण मारकाट में सुख-शान्ति नहीं दिखाई पड़ती। यह भी परिवर्तन का ही रूप है। वह जगत् की इस स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है .
व्याख्या- इस संसार के प्रातःकाल रक्त के है। मनुष्य सबेरा होते ही दूसरों का रक्त बहाने और संहार करने में लग जाता है और प्रत्येक सबेरा नई संहार-लीला लेकर सामने आता है। इसी प्रकार प्रत्येक सन्ध्याकाल चिता की अग्नि के समान दहकता है। यहाँ शून्य निश्वासों से भरा हुआ है। जहाँ भी देखी। अश्रुओं का भरा हुआ विशाल सिन्धु दिखाई देता है।
इस हिंसा और मारकाट से भरे हुए विश्व में सुख सरसों के समान थोड़ा है और शाक सुमेर के समान विशाल है। यह संसार ही संसार का कंकाल बना हुआ है। अर्थात् मनुष्य ही मनुष्य का संहारक है। इस विषम स्थिति में यहाँ आवरण-रोदन व्यर्थ है। यहाँ शान्ति और सुख कहाँ है, वह तो इस मारकाट और हिंसा के विश्व से बाहर ही मिल सकता है। विश्व की इस विषम स्थिति को देखकर हृदय से भीषण आहें निकल पड़ती है।
विशेष- (1) यहाँ विश्व की हिंसा और रक्तपात अर्जित स्थिति का यथार्थ बिम्ब प्रस्तुत हो गया है।
( 2 ) अलंकार रूपक । ‘सुख सरसों शोक सुमेरु’ में उपमा ।
नित्य का यह अनित्य नर्तन,
अचिर में चिर का अन्वेषण
अतल से एक अकूल उमंग,
विवर्तन जग, जग व्यावर्तन;
विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन !
सृष्टि की उठती तरल तरंग
उमड़ शत-शत बुद्बुद संसार
बूड़ जाते निस्सार ।
बना सैकत के तट अतिवात
गिरा देती अज्ञात ।।
शब्दार्थ – नित्य ब्रह्म -अनित्य भौतिक संसार , नर्तन = नृत्य | विवर्तन = भ्रम ।व्यावर्तन = भ्रम का मिट जाना। अचिर नश्वर – अन्वेषण खोज। अकूल- तटविहीन, सैकत- बालू। अतिवात – आँधी।
प्रसंग -प्रस्तुत प्रसंग में कवि संसार में दुःख ही दुःख होने की बात कहकर जगत् का स्वरूप स्पष्ट करता है।
व्याख्या- कवि कहता है कि इस जगत् का निर्माण ब्रह्म के अनित्य नृत्य के कारण हुआ है। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का नृत्य तो यही जगत् है। ब्रह्म तो नित्य है, किन्तु जगत् नश्वर है। यह जगत् ब्रह्म की गति है, पर मिथ्या है। हम जगत् के मिथ्या स्वरूप की ओर आकृष्ट होते हैं, किन्तु मिथ्या भ्रम के दूर हो जाने पर हमें उसकी नश्वरता का ज्ञान हो जाता है। हम इस विश्व या जगत् में ब्रह्म को खोजते-फिरते हैं, परन्तु ब्रह्म के चिर स्वरूप को पहचान नहीं पाते। यही विश्व का तत्वपूर्ण दर्शन है।
कवि जगत् का सृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार लहर सागर से उठती है और उसमें सैकड़ा बुद्बुद डूब जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म की आकांक्षा होने पर इस जगत् का निर्माण होता है और उसकी इच्छा में ही सैकड़ों जगत् नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं। यह सब उसी प्रकार होता है। जिस प्रकार आधी-बालू की दीवार को अचानक गिरा देती है।
विशेष- (1) रस्सी में सर्प का भ्रम होने को विवर्तन कहते हैं और साँप का पुनः रस्सी में विलीन हो जाना व्यावर्तन है। सृष्टि का क्रम भी इसी प्रकार है। कवि ने भारतीय दर्शन के इसका चित्रण किया है।
(2) अलंकार- सम्पूर्ण छन्द में दृष्टान्त अनुरूप
एक छवि के असंख्य उड्डुगन,
एक ही सब में स्पंदन;
एक छवि के विभात में लीन,
एक विधि के रे नित्य अधीन !
एक ही लोल लहर के छोर
उभय सुख दुःख, निशि भोर;
इन्हीं से पूर्ण त्रिगुण संसार,
सृजन ही है, संहार ।
शब्दार्थ- उडुगन = तारे। स्पंदन – चेतना. विभात- प्रभात, लोच – चंचल ।
प्रसंग –कवि जगत् के विवर्तन और व्यावर्तन होने की बात कहने के पश्चात् संसार में सभी कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानता है।
व्याख्या- पन्तजी कहते हैं कि संसार में एक ही सत्ता सभी में विद्यमान है। तारों की छवि भी उसी सत्ता की छवि है। सभी में जो कम्पन व चेतना है, वह उसी सत्ता की है। प्रभात में वे सभी तारे विलीन हो जाते हैं जिससे ज्ञात होता है कि वे सभी एक ही ईश्वर के अधीन हैं।
कवि सुख-दुख की व्याख्या करता हुआ कहता है कि जिस प्रकार लहर के उत्थान और पटन दो छोर होते हैं, उसी प्रकार सुख और दुःख प्रभात व रात्रि उस सत्ता के दो छोर हैं। यह त्रिगुणात्मक संसार इन्हीं सुख-दुःख और प्रभात-रात्रि से पूर्ण होता है। एक का सृजन होता है और दूसरे का नाश। इसीलिए कवि सृजन को ही संहार कहता है।
विशेष-(1) कवि ने अद्वैत के स्तर से अपनी रहस्य-भावना को स्पष्ट किया है। (2) अलंकार- छेकानुप्रास अलंकार की घटा व्याप्त है।
मूँदती नयन मृत्यु को रात
खोलती नव जीवन की प्रात,
शिशिर की सर्वप्रलयकर वात,
बीज बोती अज्ञात !
म्लान कुसुमों की मृदु मुसकान,
फलों में फलती फिर अम्लान;
महत् है, अरे आत्मबलिदान,
जगत् केवल आदान-प्रदान ।
शब्दार्थ- शिशिर – ऋतु विशेष, सर्वप्रलयकर- सभी कुछ नष्ट करने वाला, वान-हवा, म्लान- कुम्हलाये।
प्रसंग- कवि सारे जगत् में एक ही ब्रह्म की सत्ता मानकर सुख-दुःख का एक ही लहर के दो किनारे मानता है। इसीलिए वह सृजन को ही संहार कहता है।
व्याख्या- पन्तजी कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि की समाप्ति पर प्रभात होता है, उससे प्रकार मृत्यु के पश्चात् नवजीवन प्राप्त होता है। कवि कहता है संहार के बाद सृजन उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार शिशिर की तेज वायु सभी कुछ नष्ट कर देती है, किन्तु बीजों को चारों और फैलाकर सृजन का प्रारम्भ भी करती है।
कवि आगे कहता है कि पुष्प कुम्हला जाते हैं तो उनकी म्लान मुस्कान फलों के रूप में प्रकट होकर पुन: अम्लान हो जाती है। कवि कहता है कि आत्म-बलिदान का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि उससे नवीन सृष्टि का सृजन होता है। जगत् में तो कर्म और फल का आदान-प्रदान मात्र है और कुछ नहीं।
विशेष-(1) दार्शनिकता के कारण कथन प्रभावशाली बन पड़ा है।
(2) अलंकार- रूपक, उल्लेख तथा छेकानुप्रास
एक ही तो असीम उल्लास
विश्व में पाता विविधाभास;
शांत अंबर में नील विकास।
तरल जलनिधि में हरित विलास
वही उर उर में प्रेमोच्छ्वास,
काव्य में रस, कुसुमों में वास;
अचल तारक पलकों में हास,
लोल लहरों में लास !
विविध द्रव्यों में विविध प्रकार
एक ही मर्म मधुर झंकार।
शब्दार्थ- असीम- सीमाहीन, विविधाभास- विविध रूप। हरित- हरा ,विलास- क्रीड़ा प्रेमोच्छ्वास – प्रेम का उच्छ्वास . वास – सुगन्धित ,लास – नृत्य।
प्रसंग – पन्तजी सृजन और संहार को दार्शनिक भित्ति से समझाते हुए कहते हैं कि संहार होने पर सृजन का होना अवश्यम्भावी है।
व्याख्या- कवि कहता है कि इस विश्व में केवल एक ही व्यापक उल्लास है, जो विविध रूपों में अभिव्यक्त होता है। समुद्र में तरल हरीतिमा की क्रीड़ा व शांत आकाश की नीलिमा का विकास उसी का रूप है। वह उल्लास ही प्रत्येक हृदय में प्रेम का रूप धारण करता है। कविता में रस, पुष्पों में सुगन्धि, तारों की अचल पलकों की मुसकान और चंचल लहरों का नृत्य उसी का अभिव्यक्त रूप है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में वह भिन्न रूप धारण करता है। जिस प्रकार संगीत की एक लय भिन्न-भिन्न ध्वनियों को प्रकट करती है, उसी प्रकार एक सत्ता भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अभिव्यक्ति होती है।
विशेष – (1) ‘ उल्लास’ शब्द में सत् चित् व आनन्द तीनों रूप हैं। (3) ‘लास’ में भयानक रस का संकेत है।
वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप
हृदय में बनता प्रणय अपार;
लोचनों में लावण्य अनूप,
लोक सेवा में शिव अविकार
स्वर में ध्वनित मधुर, सुकुमार,
सत्य ही प्रेमोद्गार;
दिव्य सौंदर्य, स्नेह साकार
भावनामय संसार!
स्वीय कर्मों ही के अनुसार
एक गुण फलता विविध प्रकार;
कहीं राखी बनती सुकुमार
कहीं बेड़ी का भार !
शब्दार्थ- प्रज्ञा – बुद्धि, ब्रह्म , लोचन- नेत्र, लावण्य- सुन्दरता । अनूप = अद्वितीय। शिव – कल्याणकारी ,अविकार- दोषहीन ।
प्रसंग-पन्तजी कहते हैं कि एक नित्य ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से होती है।
व्याख्या-कवि कहता है कि ब्रह्म का वह सत्य स्वरूप ही हृदय में अपार प्रेम का रूप धारण करता है। वही नेत्रों में अद्वितीय सौन्दर्य बनता है और लोक सेवा में वही विशुद्ध और कल्याणकारी शिव बनता है। यहाँ प्रज्ञा का अर्थ बुद्धि लेकर भी वर्णन किया जा सकता है। ब्रह्म का यह स्वरूप ही स्वर में मधुर व सुकुमार ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, वह सत्य ही प्रेम का उद्गार बनता है। वही दिव्य सौन्दर्य, साकार स्नेह और भावनामय संसार की सृष्टि करता है। कवि आगे कहता है कि अपने कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। एक रस्सी कहीं तो राखी बन जाती है और कहीं वही बेड़ी का भार बन जाती है।
विशेष-(1) ब्रह्म की एक सत्ता का प्रतिपादन है। (2) अलंकार- उल्लेख एवं दृष्टान्त ।
कामनाओं के विविध प्रहार
छेड़ जगती के उर के तार,
जगाते जीवन की झंकार,
स्फूर्ति करते संचार,
चूम सुख दुःख के पुलिन अपार
छलकती ज्ञानामृत की धार !
शब्दार्थ- कामनाओं -अभिलाषाओं , स्फूर्ति – शक्ति , संचार -उत्पन्न , पुलिन- किनारे
प्रसंग- पन्तज़ी ब्रह्म से एक संज्ञा की अभिव्यक्त के रूप में ही जगत् को मानते हैं।
व्याख्या- कवि कहता है कि हृदय में अभिलाषाओं के जागृत होने पर मनुष्य उसी प्रकार कर्म करता है, जिस प्रकार इच्छा के जाग्रत होने पर वह वीणा के तारों को छोड़कर क करता है। उसके इन कर्मों से ही उसे शक्ति प्राप्त होती है तब वह उन कर्मा के कारण सुख दुःख के किनारों को छूता हुआ आगे बढ़ता है और ज्ञानामृत की धारा की प्राप्त कर लेता है।
विशेष- (1) कवि ने यहाँ सुख-दुःख के समन्वय को जीवन के लिए आवश्यक माना है।
(2) अलंकार – रूपक।
पिघल होंठों का हिलता हास
दृगों को देता जीवन-दान,
वेदना ही में तपकर प्राण
दमक दिखलाते स्वर्ण हुलास
तरसते हैं हम आठों याम,!
इसी से सुख अति सरस, प्रकाम;
झेलते निशिदिन का संग्राम
इसी से जय अभिराम;
अलभ है इष्ट, अतः अनमोल,
साधना ही जीवन का मोल!
शब्दार्थ- हास -हँसी, जीवन- जिन्दगी, पानी. हुलास -प्रसन्नता वाम- पहर। प्रकाम-बोधित, अभिराम- सुन्दर ,अलभ -जो प्राप्त न हो सके। इष्ट -वांछित वस्तु ।
प्रसंग – पन्तजी कहते हैं कि मनुष्य अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कर्म करता है और इसीलिए सुख-दुख झेलता है।
व्याख्या – कवि कहता है कि ओठों की हँसी रुदन के आँसुओं में बदल जाती है। ये आँसू ही उसे फिर जीवन प्रदान करते हैं। वेदना की अग्नि में प्राण तपकर स्वर्ण की भाँति स्वच्छ हो जाते हैं और तन-मन-सुख से भर उठता है।
कवि कहता है कि हम प्रत्येक पल तरसते रहते हैं। यही कारण है कि सुख हमारे लिए सरस और वांछित है। हम दिन-रात संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए जय हमारे लिए मनोहर है। सुख को प्राप्ति अलभ्य है, इसीलिए वह वांछित है। इस संघर्ष के पश्चात् ही सुख की प्राप्ति के कारण वह अमूल्य है और उसका मूल्य केवल जीवन की साधना है। तात्पर्य यह है कि बिना साधना के सुख की प्राप्ति सम्भव नहीं है।
विशेष- (1) ‘जीवन’ में श्लेष है।
(2) अलंकार- रूपक तथा दुःख का मूल्य बताया गया है।
बिना दुख के सब सुख निस्सार,
बिना आँसू के जीवन भार;
दीन दुर्बल है रे संसार,
इसी से दया, क्षमा औं प्यार !
आज का दुख, कल का आह्लाद,
और कल का सुख, आज विषाद;
समस्या स्वप्न मूढ़- संसार
पूर्ति जिसकी उस पार;
शब्दार्थ- निस्सार -थोथा, व्यर्थ .आहाद- सुख, विषाद -दुख. गतिक्रम-गतिशील। हास- पतन।
प्रसंग- पन्तजी सुख को अमूल्य इसलिए बताते हैं कि वह अलम्भ है, किन्तु साधना के बाद मिलता है, इसलिए दुख को भी महत्व देते हैं।
व्याख्या- कवि कहता है कि बिना दुख प्राप्त किए सुख थोथा है, क्योंकि बिना दुख के हमें उसका मूल्य ज्ञात नहीं होगा। बिना आँसू आये जीवन भार हो जाता है, क्योंकि जीवन में एक रसता रहती है, जो भार स्वरूप है। संसार दीन और दुर्बलों से भरा पड़ा है, इसी कारण दया, क्षमा और प्यार की आवश्यकता और उसका महत्व है।
आज का जो दुःख है, वही कल सुख में परिवर्तित हो जाएगा। कल जो हमने सुख प्राप्त किया था, वही आज दुख में बदल गया इसीलिए संसार एक गहरी समस्या और रहस्य-गृढ़ स्वरूप बन गया है जिसकी पूर्ति उस पार है अर्थात् इस भौतिक जगत् में सुख-दुख का क्रम चलता ही रहेगा। जीवन का अर्थ है निरनतर विकास करते जाना और मृत्यु का अर्थ है गतिहीन बना देना।
विशेष-(1) कथनों की पिछली पुनरुक्ति होने से कविता में दोष आ गया है।
हमारे काम न अपने काम,
नहीं हम, जो हम ज्ञात;
अरे, निज छाया में उपनाम
छिपे हैं हम अपरूप ।
गँवाने आए हैं अज्ञात
गँवाकर पाते स्वीय स्वरूप
शब्दार्थ– उपनाम -वास्तविक नाम के अतिरिक्त, अपरूप- अवास्तविक, निराकार।
प्रसंग – पन्तजी सुख-दुख व मृत्यु जीवन के क्रम को स्पष्ट करने के बाद इस भौतिक देह के बारे में बताते हैं।
व्याख्या – कवि कहता कि हम जो कार्य करते हैं, वे वस्तुतः हमारे कार्य नहीं हैं। वे तो किसी और के कार्य हैं जो हमें साधन बनाकर करा रहा है। हम अपने को जो कुछ समझते हैं, वह हम नहीं हैं। हम तो वास्तविक रूप के पीछे उपनाम के समान है। हमारा सत्य स्वरूप तो छिपा हुआ है। हमको यह भी पता नहीं कि हम क्या गँवाने आये हैं, किन्तु इस शरीर को गँवाकर हम अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त करते हैं।
विशेष- (1) कवि ने भारतीय दार्शनिक विचारधारा के अनुकूल जीव और जगत् का वर्णन किया है।
जगत की सुन्दरता का चाँद
सजा लांछन को भी अवदात;
सुहाता बदल, बदल, दिन-रात,
नवलता ही जग का आह्लाद।
शब्दार्थ- लांछन -कलंक, दोष ,अवदात- उज्ज्वल, सुहाता- शोभा देता है। नवलता नवीनता, आह्वाद= प्रसन्नता
प्रसंग- इस छन्द में कवि स्पष्ट करता है कि सुख-दुख सुन्दरता का विकास होता है। परिवर्तन में ही संसार की सुन्दरता का विकास होता है.
व्याख्या– संसार की सुन्दरता का चन्द्रमा लांछन को सजाकर भी उज्ज्वल रहता है। चन्द्रमा में कलंक होता है। परन्तु वह उज्ज्वल प्रकाश बिखेरता है। चन्द्रमा प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक अपने को घटाता रहता है और अमावस्या एवं प्रतिपदा को सर्वथा अस्तित्वहीन हो जाता है। अपने इस रूप में वह कलंक को धो देता है और द्वितीय के चन्द्रमा के रूप में अपना उज्ज्वल रूप सामने लाकर नव विकास करता है। दिन-रात की शोभा भी उनके परिवर्तन में हो है। दिन के पश्चात् रात और रात के पश्चात् दिन का परिवर्तन चक्र चलता रहता है और इसी में उनका सौन्दर्य निखरता है। इस प्रकार परिवर्तन ही सबसे बड़ी प्रसन्नता और आह्लाद है।
विशेष- (1) ‘परिवर्तन को कवि विश्व के विकास और नवलता का कारण मानता है।
(2) अलंकार – ‘सुन्दरता का चाँद’ में रूपक तथा’ लांछन में उज्ज्वल’ में विरोधाभास
स्वर्ण शैशव स्वप्नों का जाल,
मंजरित यौवन, सरस रसाल;
प्रौढ़ता, छाया वट सुविशाल,
स्थविरता, नीरव सायंकाल
यही विस्मय का शिशु नादान
रूप पर मँडरा, बन गुंजार;
प्रणय से बिंध, बंध चुन-चुन सार,
मधुर जीवन का मधुकर पान;
साध अपना मधुमय संसार
डुबा देता निज तन, मन, प्राण !
एक बचपन ही में अनजान
जागते, सोते, हम दिन रात;
वृद्ध बालक फिर एक प्रभात
देखता नव्य स्वप्न अज्ञात;
मूँद प्राचीन मरन
खोल नूतन जीवन !
शब्दार्थ- शैशव- बचपन, मंजरित -बौर से युक्त, रसाल- रसमय आम, नादान= अंजान ,नव्य= नया, स्थविरता- वृद्धावस्था
व्याख्या-जीवन में निरन्तर परिवर्तन चक्र चलता रहता है। शिशुरूप सुनहरे शैशव को लेकर मनुष्य पृथ्वी पर अवतरित होता है। वह शैशव नाना प्रकार के स्वप्न-जाल से युक्त होता है।
शैशव यौवन में भी परिवर्तित हो जाता है। सरल रसाल की तरह यौवन मंजरित हो उठता है। यौवन की रसमय उद्दाम भावनायें जीवन को सरस बना देती है। यौवन की मादकता प्रौढ़ता में परिवर्तित हो जाती है। उसकी प्रौढ़ता विशाल छाया-वट के समान प्रसारित होती है। इसके पश्चात् वृद्धावस्था की संध्या नीरव शान्ति का प्रसार करती है।
मानव जो विस्मय से भरा हुआ नादान शिशु-सा पृथ्वी पर जन्म लेता है और जो युवावस्था प्राप्त करके रूप-सौन्दर्य पर मँडराता है तथा भ्रमर के समान गुंजार करता हुआ किसी के प्रणय बंध जाता है और मधुर जीवन सार चुन-चुनकर मधुपान करता है। इस प्रकार वह अपना मधुमय संसार बसाकर उसमें अपने तन-मन और प्राणों को निमग्न कर देता है। परन्तु वृद्धावस्था की संध्या आकर उसे अपने में लीन कर मृत्यु को सौंप देती है। इस प्रकार मानव का जीवन शैशव से लेकर मृत्युपर्यन्त परिवर्तन की गाथा है।
मनुष्य बचपन की अज्ञानता में ही दिन-रात सोता-जागता रहता है। वह बालक से वृद्ध होकर मृत्यु प्राप्त करता है और पुन: उसके जीवन का प्रभात होता है। अर्थात् वह शिशुरूप में जन्म लेता है और शैशव के रूप में भव्य स्वप्न लेकर पुनः अवतरित होता है।
विशेष-(1) यहाँ पन्तजी ने मानव जीवन दर्शन की तत्वपूर्ण विवेचना की है। शैशव • मानव जीवन का सवेरा और मृत्यु संध्या है। जिस प्रकार प्रात: और संध्या के क्रम में सृष्टि निरन्तर चलती रहती है। इसी प्रकार शैशव, यौवन, बुढ़ापा, मृत्यु और मृत्यु के पश्चात् शैशव, यौवन, ये के क्रम में मानव-जीवन चलता रहता है। यहाँ पन्तजी ने आवागमन के प्रति आस्था प्रकट की है।
(2) अलंकार-‘सवर्ण शैशव’ में ‘ स्वप्नों के जाल’ का आरोप, होने से रूपक। ‘मंजरित यौवन’ में ‘सरस रसाल’ का आरोप तथा ‘ प्रौढ़ता’ में ‘छाया-वट’ का आरोप तथा ‘ स्थविरता’ (वृद्धावस्था) में ‘संध्याकाल’ का आरोप होने से रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण
\
विश्वमय है परिवर्तन !
अतल से उमड़ अकूल अपार
मेघ-से, विपुलाकार;
दिशावधि में पल विविध प्रकार
अतल में मिलते तुम अविकार !
अहे अनिर्वचनीय ! रूप धर भव्य भयंकर,
इन्द्रजाल-सा तुम अनन्त में रचते सुन्दर;
गरज-गरज, हँस-हँस, चढ़-गिरा, छा- ढा, भूअंबर,
करते जगती को अजस्त्र जीवन से उर्वर;
अखिल विश्व की आशाओं का इन्द्रचाप वर
अहे तुम्हारी भीम भृकुटि पर
अदका निर्भर |
शब्दार्थ – विश्वमय = समस्त विश्व में व्याप्त विश्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अतल -पाताल, बहुत गहरे ,अकूल- कूलों से रहित विपुलाकार- बहुत बड़ा आकार ,अविकार =समस्त विकारों से रहित, इन्द्रजाल= जादू. अम्बर =आकाश. उर्वर =उपजाऊ।
प्रसंग -यहाँ कवि परिवर्तन को विश्वरूप देता हुआ उसे समस्त संसार का आधार कह रहा है.
व्याख्या – हे परिवर्तन ! तुम विश्व रूप सृष्टिकर्ता हो और समस्त विश्व में व्या तुम कभी अतल से उमड़कर कुल-रहित प्रबल धारा के समान प्रवाहित होते हो और कभी अ मेम सा विपुलाकार रूप धारण करते हो। तुम दिशा की अवधि में विविध प्रकार से पालित होते हो और समस्त विकारों से रहित होकर अतल में मिल जाते हो।
हे परिवर्तन ! तुम अनिर्वचनीय हो। तुम पूरे इन्द्रजाली हो। कभी भव्य और कभी भयंका रूप धारण करके तुम अनन्त में सुन्दर इन्द्रजाल रचते हो तुम गर्जना करते हुए ह चढ़ते और गिरते हुए पृथ्वी और आकाश को ढाते रहते हो, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा पृथ्वी जीवन से उर्वर होती रहती है। तुम सम्पूर्ण भीम भृकुटियों पर ही अटका हुआ निर्भर है।
विशेष- (1) यहाँ कवि ने परिवर्तन की विश्वमय, विश्व-नियंता के रूप में चित्रण किया है।
(2) अलंकार- अकूल अपार’ में छेकानुप्रास परिवर्तन की समता विपुलाकार मेघ होने में उपमा ‘इन्द्रजाल सा तुम’, ‘गरज-गरज अंबर’ में अनुप्रास और नाद-सौन्दर्य ‘आशाओं का इन्द्रचाप वर’ में रूपक
एक औ’ बहु के बीच अजान
घूमते तुम नित चक्र समान;
जगत् के उर में छोड़ महान्
गहन चिह्नों में ज्ञान !
परिवर्तित कर अगणित नूतन दृश्य निरन्तर
अभिनय करने विश्व मंच पर तुम माया कर !
जहाँ हास के अधर, अश्रु के नयन करुणतर,
पाठ सीखते संकेतों में प्रकट, अगोचर;
शिक्षास्थल यह विश्व मंच, तुम नायक नटवर,
प्रकृति नर्तकी सुधर
अखिल में व्याप्त सूत्रधर
शब्दार्थ- निरन्तर अविराम रूप से मायाकर मायाजाली ह्रास के अधर प्रसन्नता और आनन्द अगोचर अदृश्य ।
प्रसंग- इस छन्द में पन्तजी ने विश्व को मंच बताकर परिवर्तन को सूत्राधार के रूप में के प्रस्तुत किया है।
व्याख्या – हे मायामय परिवर्तन। तुम एक और अनेक व्यष्टि और समष्टि के बीच में निरन्तर अदृष्ट रूप में घूमते रहते हो। जिस प्रकार चक्र घूमता है, उसी प्रकार तुम विश्व का नियति चक्र बनकर उसे संचालित करते रहते हो। तुम चक्र के समान घूमते हुए जगत के हृदय पर, अपने चिह्न छोड़ते चलते हो। तुम अपने परिवर्तन चक्र की गति में निरन्तर अगणित नूतन दृश्य प्रस्तुत करते रहते हो। तुम पूरे इन्द्रजाली बने हुए विश्व के मंच पर अभिनय करते रहते हो।
इस विश्व के रंगमंच पर कहीं अधरों पर हास लिए हुए आनन्द और प्रसन्नता के दृश्य आते रहते हैं और कहीं अश्रु भरे हुए मनुष्य अत्यन्त करुणा का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह विश्व मंच शिक्षा स्थल है, जिस पर तुम अगोचर रूप से निरन्तर नृत्य करते रहते हो। इस सुख-दु:ख से भरे हुए विश्व-मंच का दर्शक मनुष्य है। उसे तुम अपने संकेतों से शिक्षा देते हो, हे नटवर नायक परिवर्तन! तुम सुन्दर प्रकृति नदी के साथ नृत्य करते हो और अविरल विश्व में व्याप्त उसके सूत्रधार हो।
विशेष- (1) परिवर्तन को विश्व को नियंत्रित करने वाली महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है,
(2) अलंकार परिवर्तन की समता चक्र से होने से उपमा ‘विश्व-मंच’ में ‘परिवर्तन’ किया गया है। ‘नायक नटवर’ और ‘सूत्रधार’ का आरोप होने से एवं प्रकृति में नर्तकी का आरोप होने से रूपक तथा मानवीकरण। (3) जहाँ ह्रास के अधर करुणतर’ में लाक्षणिकता।
हमारे निज सुख, दुख, निःश्वास,
तुम्हें केवल परिहास;
तुम्हारी ही विधि पर विश्वास
हमारा चिर आश्वास !
ऐ अनन्त हृत्कंप तुम्हारा अविरत स्पंदन,
सृष्टि शिराओं में संचारित करता जीवन;
स्रोत जगत् के शत-शत नक्षत्रों से लोचन,
भेदन करते अंधकार तुम जग का क्षण-क्षण;
सत्य तुम्हारी राज, यष्टि, सम्मुख नत त्रिभुवन
भूप, अकिंचन,
अटल शास्ति नित करते पालन।
शब्दार्थ – परिहास= हँसी, आश्वास= सान्त्वना तसल्ली। हृत्कंप हृदय को = कंपायमान करने वाला। अविरत= निरन्तर, लोचन= नेत्र, राज-यष्टि ,राज-दंड। यष्टि= लाठी-डंडा । नत =झुका हुआ। शास्ति =शासन।
प्रसंग- यहाँ कवि परिवर्तन को विश्व की नियंत्रिका (नियति) शक्ति बताता हुआ उसे अखिल विश्व का शासक कहता है।
व्याख्या- हे परिवर्तन ! तुम हमारी नियति हो, हमारे व्यक्तिगत सुख, दुःख और निःश्वास तुम्हारे लिए परिहास मात्र हैं। परन्तु तुम्हारी विधि पर विश्वास करके ही हम सान्त्वना पाते हैं। तुम अनन्त हृत्कंप हो। तुम्हारा निरन्तर स्पन्दन सृष्टि की शिराओं में जीवन-संचार करता रहता है। तुम संसार के नेत्रों को शत-शत नक्षत्रों के समान खोल देते हो और इस प्रकार एक क्षण में तुम संसार के अन्धकार का भेदन कर देते हो। सत्य ही तुम्हारा राजदण्ड है, जिसके समक्ष त्रिभुवन के भूप नत हो जाते हैं और वे अकिंचन बने हुए निरन्तर तुम्हारे शासन का पालन करते हैं।
विशेष- अलंकार -(1) मानवीकरण, उल्लेख, ‘सृष्टि-शिराओं’ एवं ‘ सत्य तुम्हारी राज-यष्टि’ में रूपक। ‘शत्-शत्’ और ‘ क्षण-क्षण’ में पुनरुक्तिप्रकाश तथा ‘ नक्षत्रों से लोचन’ में उपमा।
तुम्हारा ही अशेष व्यापार,
हमारा भ्रम, मिथ्याहंकार;
तुम्हीं में निराकार साकार,
मृत्यु जीवन सब एकाकार !
अहे महाबुद्धि! लहरों से शत लोक, चराचर
क्रीड़ा करते सतत तुम्हारे स्फीत वक्ष पर
तुंग तरंगों से शत युग, शत-शत कल्पांतर
उगल,महोदर में विलीन करते तुम सत्वर ।
शत सहस्त्र रवि शशि, असंख्य ग्रह उपग्रह, उडुगन
जलते बुझते हैं स्फुलिंग-से तुम में तत्क्षण;
अचिर विश्व में अखिल-दिशावधि, कर्म, वचन, मन,
तुम्हीं चिरंतन
अहे विवर्तनहीन विवर्तन!
शब्दार्थ- अशेष =सम्पूर्ण ,मिथ्याहंकार =अपनी शक्ति का झूठा अहंकार, महाबुधि= महासागर। स्फीत = उठे हुए। तुग= ऊँची सत्वर= शीघ्र ,उडुगन= तारागण ,स्फुलिंग =चिंगारी ,अचिर =नश्वर, विवर्तनहीन विवर्तन = परिवर्तन से रहित परिवर्तन- के चक्र में ही सृष्टि क्रम निरन्तर चलता रहता है, इसीलिए उसे कवि ने विवर्तनहीन विवर्तन कहा है।
प्रसंग – इस छन्द में कवि ने परिवर्तन को समस्त सृष्टि को उत्पन्न करने और फिर उसे अपने में विलीन कर लेने वाली महाशक्ति के रूप में चित्रित किया है ।
व्याख्या- इस सृष्टि के उत्थान पतन, सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश तथा मेरे समस्त कार्य-कलाप तुम्हारे ही सम्पूर्ण व्यापार का प्रतिफल हैं। यदि उसे मैं अपना कहूँ तो यह मेरा मिथ्या अहंकार मात्र ही होगा। तुम्हीं निराकार और साकार दोनों ही में समाये हुए हो और मृत्यु तथा जीवन दोनों तुम्हीं में एकाकर हो रहे हैं।
हे परिवर्तन ! तुम वह महासागर हो, जिसमें शत-शत लोक लहरों के समान उठते और विलीन होते रहते हैं। यह चराचर विश्व तुम्हारे ऊपर उठे हुए वक्षस्थल पर निरन्तर क्रीड़ा करता रहता है। तुम अपनी उत्तुंग तरंगों से शत-शत युग एवं कल्पों की सृष्टि करते हो और शीघ्र ही उनको अपने महाकालरूपी उदर में विलीन कर लेते हो।
शत सहस्त्र शमिश, असंख्य ग्रह, उपग्रह और तारागण तुम में ही चिंगारियों के समान, जलते-बुझते रहते हैं। यह अखिल विश्व, दिशावधि, कर्म, वचन, मन आदि सभी कुछ नश्वर हैं। इनमें केवल मात्र तुम्हीं चिरंतन हो। तुम परिवर्तनहीन होने पर भी परिवर्तन हो । तुम परिवर्तन के द्वारा नवीनता की सृष्टि करते हो।
विशेष- (1) परिवर्तन को सृष्टि के जन्म, विकास और विनाश का कारण कवि द्वारा माना है। ‘निराकार साकार’ में नाद-सौन्दर्य और ध्वन्यात्मकता व्यंजित है।
(2) अलंकार – ‘परिवर्तन’ में ‘महाबुद्धि’ का आरोप होने से रूपक, ‘जलते-झ ‘स्फुलिंग से’ में उपमा, ‘विवर्तनहीन विवर्तन’ में विरोधाभास तथा अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश ।