शब्द शक्ति व प्रकार
काव्य में रस का संचार शब्द-शक्तियों के द्वारा होता हैं। यहाँ शब्दों का विशेष महत्त्व माना गया हैं। काव्य-भाषा में वाक्यों की रचना इस बात की सूचक हैं कि उसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रकरण, प्रसंग और कवि-आशय के अनुसार हुआ हैं।
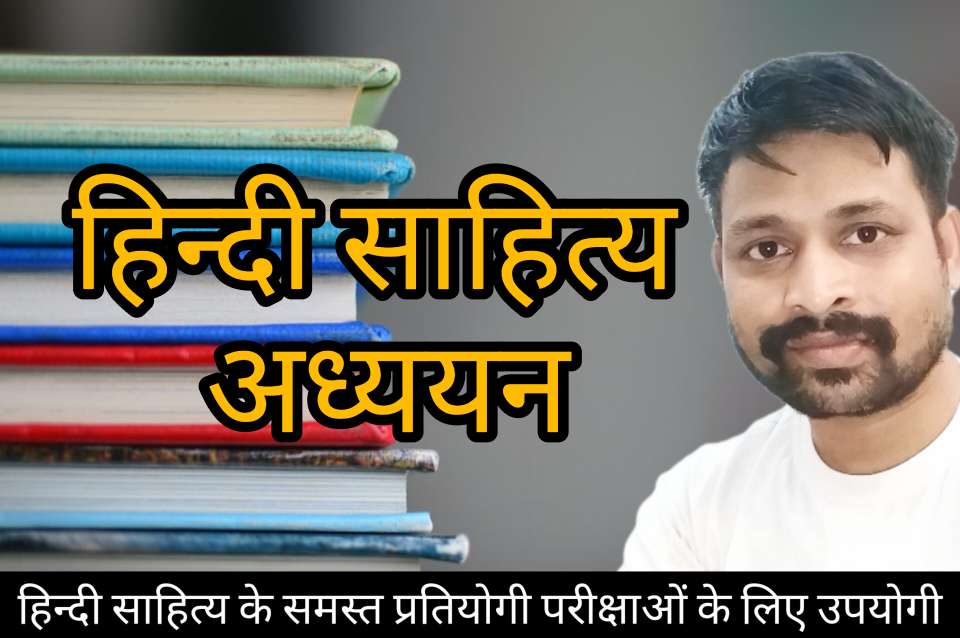
Table of Contents
शब्द शक्ति
आचार्य मम्मट ने व्यापार शब्द का और आचार्य विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया हैं।
परिभाषा
शब्द का अर्थ बोध करानेवाली शक्ति ‘शब्द शक्ति’ कहलाती है। ‘शब्द की शक्ति उसके अन्तर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार हैं।”
हिन्दी के रीतिकालीन आचार्य चिन्तामणि ने लिखा है कि ”जो सुन पड़े सो शब्द है, समुझि परै सो अर्थ”
शब्द तीन प्रकार के- वाचक, लक्षक एवं व्यंजक होते हैं तथा इन्हीं के अनुरूप तीन प्रकार के अर्थ- वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ होते हैं। शब्द और अर्थ के अनुरूप ही शब्द की तीन शक्तियाँ- अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना होती हैं।
| शब्द | अर्थ | शक्ति |
|---|---|---|
| वाचक/अभिधेय | वाच्यार्थ/अभिधेयार्थ/मुख्यार्थ | अभिधा |
| लक्षक/लाक्षणिक | लक्ष्यार्थ | लक्षणा |
| व्यंजक | व्यंग्यार्थ/व्यंजनार्थ | व्यंजना |
शब्द शक्ति के प्रकार
प्रक्रिया या पद्धति के आधार पर शब्द-शक्ति तीन प्रकार के होते हैं-
(1) अभिधा
(2) लक्षणा
(3) व्यंजना
अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबद्ध लक्ष्यार्थ का, लेकिन व्यंजना से न मुख्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, बल्कि इन दोनों से भित्र अर्थ व्यंग्यार्थ का बोध होता है।