भाषा की उत्पत्ति सिद्धांत (The Origin Theory of Language)
भाषाओं की उत्पत्ति (The Origin Theory of Language) के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन मत यह है कि संसार की अनेकानेक वस्तुओं की रचना जहाँ भगवान ने की है । भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष शब्द से हुई जिसका अर्थ है बोलना, यानि जब हमने बोलना सीखा उसी समय भाषा का भी जन्म हो गया ।
भाषा की लिखित अभिव्यक्ति पुरापाषाण काल मे हुई। तब ये सांकेतिक रूप में चित्रित की गई, और धीरे धीरे समय के साथ भाषा के चिन्हों को विकसित किया जाता रहा
भाषा की उत्पत्ति सिद्धांत (The Origin Theory of Language)
भाषा की दैवी उत्पत्ति-सिद्धान्त
- संस्कृत को ‘देवभाषा’ कहने में इसी का संकेत मिलता है।
- इसी प्रकार पाणिनी के व्याकरण ‘ अष्टाध्यायी ’ के 14 मूल सूत्र महेश्वर के डमरू से निकले माने जाते हैं।
- बौद्ध लोग ‘पालि’ को भी इसी प्रकार मूल भाषा मानते रहे हैं ।
- जैन के अनुसार अर्धमागधी केवल मनुष्यों की ही नही अपितु देव, पशु-पक्षी सभी की भाषा है।
- हिब्रू भाषा के कुछ विद्वानों ने बहुत-सी भाषाओं के वे शब्द इकट्ठे किए जो हिबू से मिलते जुलते थे । इस आधार पर यह सिद्ध किया कि हिब्रू ही संसार की सभी भाषाओं की जननी है।
यदि भाषा की दैवी उत्पत्ति हुई होती हो सारे संसार की एक ही भाषा होती तथा बच्चा जन्म से ही भाषा बोलने लगता। इससे सिद्ध होता है कि यह केवल अंधविश्वास है कोई ठोस सिद्धान्त नहीं है।
निष्कर्ष:
भाषा की उत्पत्ति ( The Origin Theory of Language ) के सम्बन्ध में दैवी सिद्धान्त तर्कसंगत नहीं है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। इसमें भाषा की उत्पत्ति की समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। हाँ, इस सिद्धान्त में यहाँ तक सच्चाई तो है कि बोलने की शक्ति मनुष्य को जन्मजात अवस्था से प्राप्त है।
भाषा की संकेत सिद्धान्त (Symbolic thoery)
- इसे निर्णय-सिद्धान्त भी कहते हैं।
- इस सिद्धान्त के प्रथम प्रतिपादक फ्राँसीसी विचारक रूसो हैं।
- संकेत सिद्धान्त के अनुसार प्रारम्भिक अवस्था में मानव ने अपने भावों-विचारों को अपने अंग संकेतों से प्रषित किया होगा । बाद में इसमें जब कठिनाई आने लगी तो सभी मनुष्यों ने सामाजिक समझौते के आधार पर विभिन्न भावों, विचारों और पदार्थों के लिए अनेक ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिए।
- यह कार्य सभी मनुष्यों ने एकत्र होकर विचार विनिमय द्वारा किया।
इस संकेत सिद्धान्त के आधार पर आगे चलकर ‘रचई’, ‘राय’ तथा जोहान्सन आदि विद्वानों ने इंगित सिद्धान्त (Gestural theory) का प्रतिपादन किया जो संकेत सिद्धान्त की अपेक्षा कुछ अधिक परिष्कृत होते हुए भी लगभग इसी मान्यता को प्रकट करता है।
समीक्षा
यह सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि इससे पूर्व मानव को भाषा की प्राप्ति नहीं हुई थी। यदि ऐसा है तो अन्य भाषाहीन प्राणियों की भाँति मनुष्य को भी भाषा की आवश्यकता का अनुभव नहीं होना चाहिए था।
निष्कर्ष :
इस सिद्धान्त में एक तो कृत्रिम उपायों द्वारा भाषा की उत्पत्ति सिद्ध करने का प्रयास किया गया है दूसरे यह सिद्धान्त पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। अतः तर्क की कसौटी पर खरा नही उतरता।
भाषा की धातु या अनुरणन सिद्धान्त (Root-theory)
- इस सिद्धान्त के मूल विचारक ‘प्लेटो’ थे।
- मैक्समूलर ने भी पहले इसे स्वीकार किया किन्तु बाद में व्यर्थ कहकर छोड़ दिया।
- इस सिद्धान्त के अनुसार संसार की हर चीज की अपनी एक ध्वनि है। यदि हम एक डंडे से एक काठ, लोहे, सोने, कपड़े, कागज आदि पर चोट मारें तो प्रत्येक में से भिन्न प्रकार की ध्वनि निकलेगी।
समीक्षा
- इस सिद्धान्त की निस्सारता या अनुपयोगिता के कारण ही मैक्समूलर ने इसका परित्याग किया था।
- इस सिद्धान्त के अनुसार आदि मानव में नये-नये धातु बनाने की सहज शक्ति का होना कल्पित किया गया है।
- यह सिद्धान्त शब्द और अर्थ में स्वाभाविक सम्बन्ध मान कर चलता है किन्तु यह मान्यता निराधार है।
- सभी भाषाएँ धातुओं से बनी हैं किन्तु चीनी आदि कुछ भाषाओं के सम्बन्ध में यह सत्य नहीं है।
- यह सिद्धान्त भाषा को पूर्ण मानता है जबकि भाषा सदैव परिवर्तन और गतिशील होने के कारण अपूर्ण ही रहती है।
- आधुनिक मान्यता के अनुसार भाषा का आरम्भ धातुओं से बने शब्दों से न होकर पूर्ण विचार वाले वाक्यों के द्वारा हुआ होगा।
निष्कर्ष :
अपने पूर्ववर्ती सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी तर्क की कसौटी पर विफल हो जाने के कारण भाषा के आरम्भ का कोई निश्चित समाधान प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः इस विषय पर विचार की पुनः आवश्यकता बनी ही रही।
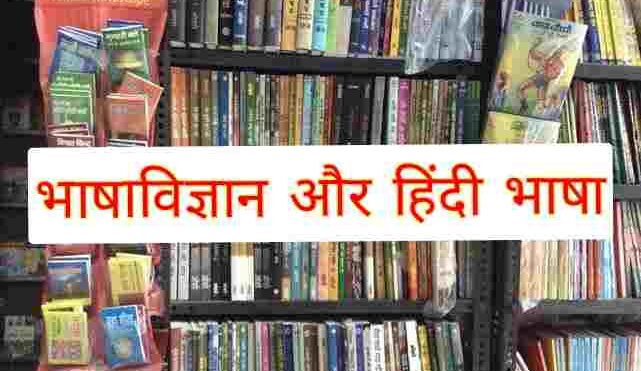
भाषा की अनुकरण सिद्धान्त (Bow & Bow Theory)
- इस सिद्धान्त को मानने वाले प्रमुख विद्वान हैं- ‘ह्निटनी’ ‘पॉल’, ‘हर्डर’ आदि।
- मैक्समूलर ने इस सिद्धान्त का उपहास करते हएु इसे (कुत्ते की ध्वनि) बॉक बॉब सिद्धान्त कहा था।
- अनुकरण सिद्धान्त में भी अनुरणन की ही भाँति कुछ प्राकृतिकक ध्वनियों के अनुकरण पर पदार्थों के नामकरण की कल्पना की गई है।
- कुछ शब्द उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं- ‘काक‘, ‘कोकिल’ ‘भौं-भौं’, ‘म्याऊँ’, ‘कुक्कर’, ‘दादुर’, ‘निर्झर’, ‘टर्राना’, ‘मर्मर’, ‘तड़तड़’, ‘कडकना’ ‘गड़गड़ाना’, ‘टपकना’, ‘चहकना’, ‘चहचहाना’, ‘हिनहिनाना’, ‘गुर्राना’, ‘काँव-काँव’, ‘टेंटें करना’, ‘चिल्लाना’, ‘गरजना’, ‘टप-टप’, आदि।
समीक्षा
विद्वानों ने इस सिद्धान्त के खण्डन के लिए निम्नलिखित तर्क दिये हैं:
- प्रसिद्ध विद्वान् ‘रेनन’ के अनुसार ध्वनियों का उत्पादन करने में मनुष्य पशु-पक्षियों से भी निकृष्ट सिद्ध होता है इसलिए यह सिद्धान्त विश्वास करने के योग्य नहीं है।
- यद्यपि कुछ भाषाओं में अनुकरणामूलक शब्द पाये जाते हैं। परन्तु इन शब्दों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती कि इनसे भाषा का उत्पन्न होना मान लिया जाए। उत्तरी अमेरिका की एक भाषा ‘अथवाकन’ में तो एक भी शब्द अनुकरणमूलक नहीं है।
- अनुकाणमूलक शब्द सभी भाषाओं में एक समान नहीं हैं उनका रूप भिन्न-भिन्न है। कुछ विद्वानों ने इसका कारण भिन्न-भिन्न भाषाओं में ध्वनियों की भिन्नता बताया है परन्तु यह स्वीकार इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ध्वनियाँ तो इस सिद्धान्त के अनुसार अनुकरण का ही परिणाम है, हाँ अनुकरण की अपूर्णता इसमें आंशिक रूप में कारण माना जा सकता है।
- अनुकरण पर बने शब्द किसी भाषा में बहुत कम संख्या में होते हैं जिनके आधार पर भाषा का अलंकरण तो हो सकता है परन्तु उन्हें पूरी भाषा के अस्तित्व का आधार नहीं माना जा सकता।
निष्कर्ष :
‘ऑटो जेस्पर्सन’ नामक विद्वान ने कहा था कि इस सिद्धान्त पर भाषा के कुछ शब्दों का निर्माण होना माना जा सकता है जो भाषा की उत्पत्ति का आंशिक आधार माने जा सकते हें, पूर्ण आधार नहीं।
भाषा की आवेश सिद्धान्त (Pooh-Pooh Theory or Interjectional theory)
- इस सिद्धान्त को मनोभावाभिव्यंजकतावाद अथवा ‘मनोरागाभिव्यंजक शब्द मूलकतावाद’ कहा जाता है।
- इस सिद्धान्त के अनुसार आदि युग में भाव को व्यंजित करने के लिए जिन ‘आहा’, ‘ओहो’, ‘फिक्’ ‘छिः’ पूह (Pooh), ‘पिश (Pish) ‘फाई’ (Fie) आदि ध्वनियों को उत्पन्न किया ।
- ‘धिक्’ से ‘धिक्कार’, ‘धिक्कारना’, ‘धिक्-धिक्’ करना आदि शब्द बने हैं ठीक इसी प्रकार सारी भाषा बनी है।
समीक्षा
इस सिद्धान्त में अनेक प्रकार की कमियाँ हैं, जैसे-
- भाव-व्यंजक शब्दों को वाक्य के पहले अलग से जोड़ा जाता है वे हमारी भषा का मुख्य अंग या सम्पूर्ण अस्तित्व नहीं है।
- ‘बेनफी’ के अनुसार इस प्रकार के शब्द भाषा की असमर्थता को प्रकट करते हैं फिर वे भाषा कैसे बन सकते हैं।
- भाषा सोच विचार कर उत्पन्न की गई ध्वनियों का व्यवस्थित रूप है परन्तु ये आवेशजनित निकलने वाले शब्द विचार और व्यवस्था से रहित होते हैं। ये तो स्वतः ही मुख से निकलने वाले आवेग हैं।
- ये शब्द जो आवेगों को प्रकट करते हैं सभी भाषाओं में एक समान रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं जैसे- पीड़ा को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी ओह, (Oh), जर्मन ‘आउ’ (Au), फ्रांसीसी ‘आहि’ (Ahi) भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग करते हैं। हिन्दी में इसके लिए ‘हाय’, ‘दैया’ आदि शब्दों का प्रयोग होता है।
निष्कर्ष :
इस सिद्धान्त के अनुसार जो थोड़े से शब्दों का समाधान हो पाता है उनका भाषा में कोई विशेष महत्त्व नहीं है।
भाषा की श्रम-ध्वनि सिद्धान्त (yo-he-ho- theory)
- हिन्दी में इसे ‘श्रमपरिहरणमूलकतावाद’ कहा जाता है।
- न्वारे (Noire) नामक प्रसिद्ध विद्वान् द्वारा इस सिद्धान्त का सूत्रपात किया गया।
- इस सिद्धान्त के अनुसार जब व्यक्ति श्रम करता है तो उसकी श्वास की गति तीव्र होने से स्वरतंत्रियों में स्वतः एक कम्पन्न होने लगता है जो कुछ स्वाभाविक ध्वनियों को उत्पन्न करता है।
- आदि मानव जब सामूहिक श्रम करते थे तो उनके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल पड़ती होंगी जैसी हम धोबियों के मुख से ‘हियो-हियो’, ‘छियो-छियो’, तथा मल्लाहों के मुख से ‘हैया हो’, हथौड़ा चलाने वाले मज़दूर के मुंह से ‘हूँ-हूँ’ की ध्वनियाँ निकलते हुए प्रायः देखते हैं।
अंग्रेज़ी के ‘हीव’ (Heave) तथा ‘हॉल’ (Houl) ‘यो-हे-हो’ ध्वनियों के द्वारा बनी हुई क्रियापद हैं।
समीक्षा
इस सिद्धान्त में निम्नलिखित त्रुटियाँ हैं-
- आवेग से उत्पन्न ध्वनियाँ निरर्थक हैं और निरर्थक ध्वनियों द्वारा किसी सार्थक भाषा को विकसित कैसे किया जा सकता है।
- ये ध्वनियाँ केवल शारीरिक श्रम को व्यक्त कर पाती है, भावों और विचारों की इनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं होती।
- इसमें जो शब्द हैं वे इतनी अल्प संख्या में हैं कि उन्हें सम्पूर्ण भाषा के विकास का आधार नहीं बनाया जा सकता।
निष्कर्ष :
इस Origin Theory of Language के आधार पर बने शब्दों से भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान प्राप्त नहीं होता।
भाषा की इंगित् सिद्धान्त (Gestural theory)
- इस सिद्धान्त में विश्वास करने वाले इसके जन्मदाता डॉ॰ राये, ‘रिचर्ड’ तथा जेहान्सन हैं।
- इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य जब पानी पीता था तो ‘पा-पा’ जैसी ध्वनि निकालती थी। जिससे ‘पिपासा’ जैसे शब्द बने।
समीक्षा
मानव अपनी ही ध्वनियों का उच्चारण करेगा यह अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता।
निष्कर्ष :
सारी भाषा की उत्पत्ति की दृष्टि से ये ध्वनियाँ बहुत अल्प हैं। इनसे भाषा-उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं होता।
भाषा की सम्पर्क सिद्धान्त (Contact theory)
प्रसिद्ध विद्वान जी. रेवेज इसके जन्मदाता हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार आदिम मानव जब समूह के सम्पर्क में आया होगा तो पहले कुछ ध्वनियाँ उसके मुंह से निकली होगी ।
इन विद्वान् के अनुसार पहले भाषा में क्रिया पद बने होंगे और बाद में अन्य शब्द।
समीक्षा
मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धान्त में कुछ तथ्य तो प्रतीत होता है परन्तु केवल इन्हीं शब्दों के द्वारा सम्पूर्ण भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का समाधान प्राप्त नहीं होता। इस सिद्धान्त में कल्पना और अनुमान का सहारा लिया गया है।
निष्कर्ष :
प्रसिद्ध विद्वान् कॉसिडी भी इस सिद्धान्त को अपूर्ण मानते हैं।
भाषा की समन्वित सिद्धान्त
ऊपर उल्लिखित अधिकांश सिद्धान्त भाषा की उत्पत्ति की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं. इसी कारण विद्वानों ने उन तीन-चार सिद्धान्तों का समन्वय करके इस समस्या का समाधान पाने की चेष्टा की है जिनमें आंशिक समाधान की मात्रा अधिक है। इस प्रकार इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है।
प्रसिद्ध विद्वान् हेनरी स्वीट (Henery Sweet) ने यही कार्य किया है। उन्होंने किसी नये सिद्धान्त को न खोज कर (क) ‘अनुकरण सिद्धान्त’ (ख) ‘आवेग सिद्धान्त’ (ग) ‘प्रतीक सिद्धान्त’ और (घ) ‘उपचार-सिद्धान्त’ का समन्वित रूप ही प्रस्तुत किया है।
समीक्षा
- ‘स्वीट के समन्वय-सिद्धान्त में यद्यपि पर्याप्त सत्य है किन्तु पूर्णतः निर्दोंष इसे भी नहीं माना जा सकता .
- भाषा की उत्पत्ति की समस्या का पूर्णरूपेण समाधान इस सिद्धान्त के द्वारा भी नहीं किया जा सकता।
निष्कर्ष
भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत-सिद्धान्त रचे गए। परन्तु वे सब के सब कल्पना और अनुमान पर अधारित होने के कारण भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वहीन सिद्ध हो चुके हैं। केवल इस प्रश्न के इतिहास की दृष्टि से ही उनका उल्लेख किया जाता है। वास्तव में अभी तक भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का कोई सर्वमान्य और उचित समाधान नहीं खोजा जा सका है।
आशा है आपको हिंदी साहित्य का यह पोस्ट (The Origin Theory of Language in Hindi ) जानकारीप्रद लगी होगी, यदि हाँ तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरुर करें और यदि इसके अतिरिक्त पोस्ट से संबन्धित आपके पास अतिरिक्त और सही जानकारियाँ हो कमेंट बॉक्स में जरुर लिखें . हम उन्हें अगली बार जरुर अपडेट करेंगे. आप से नीचे दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं